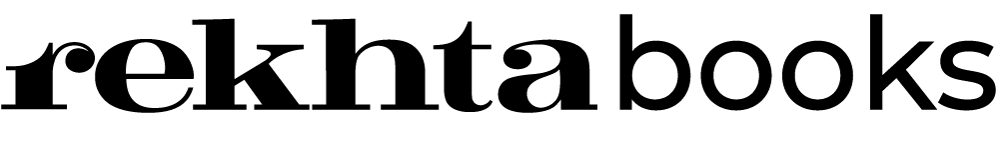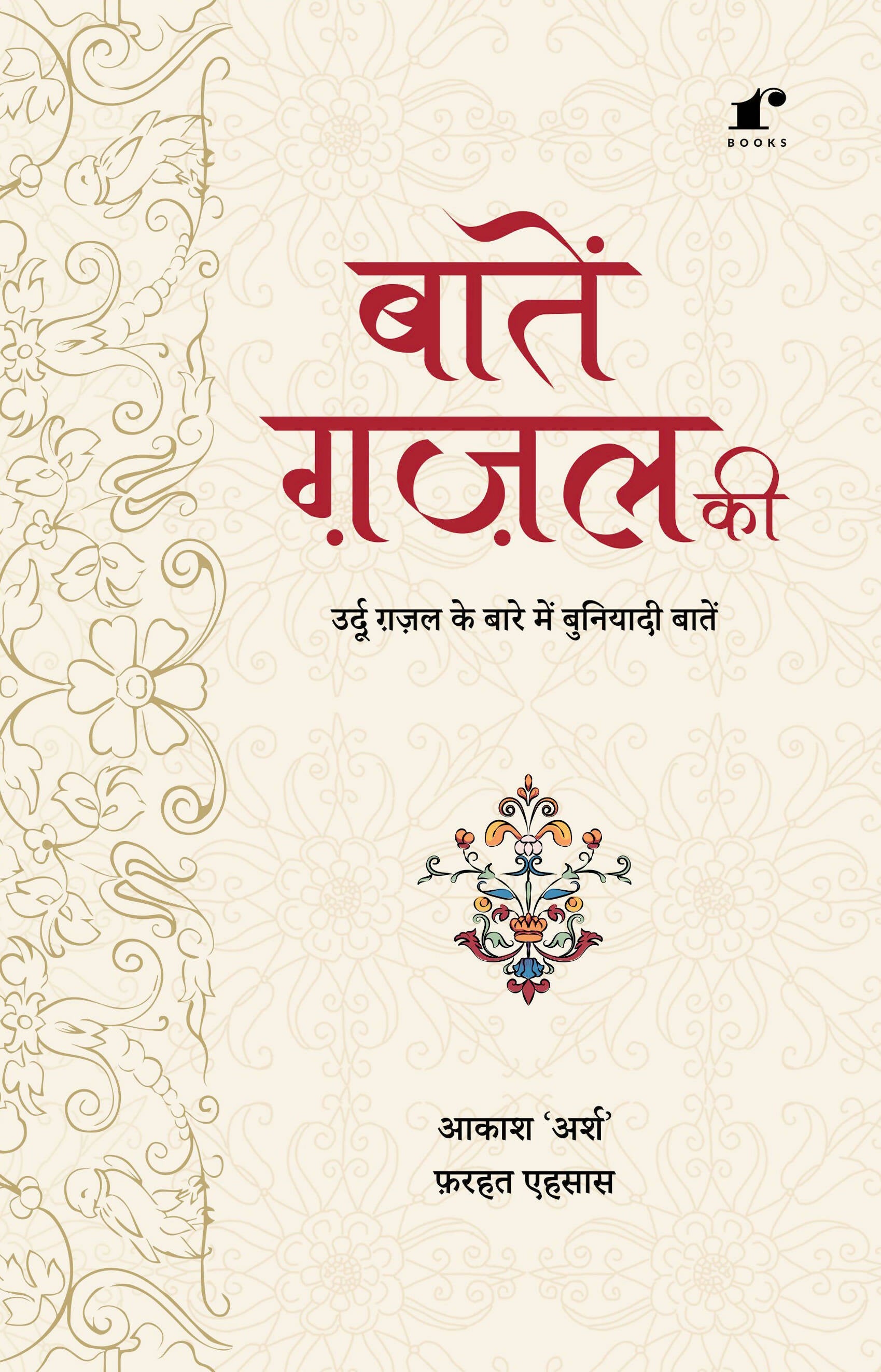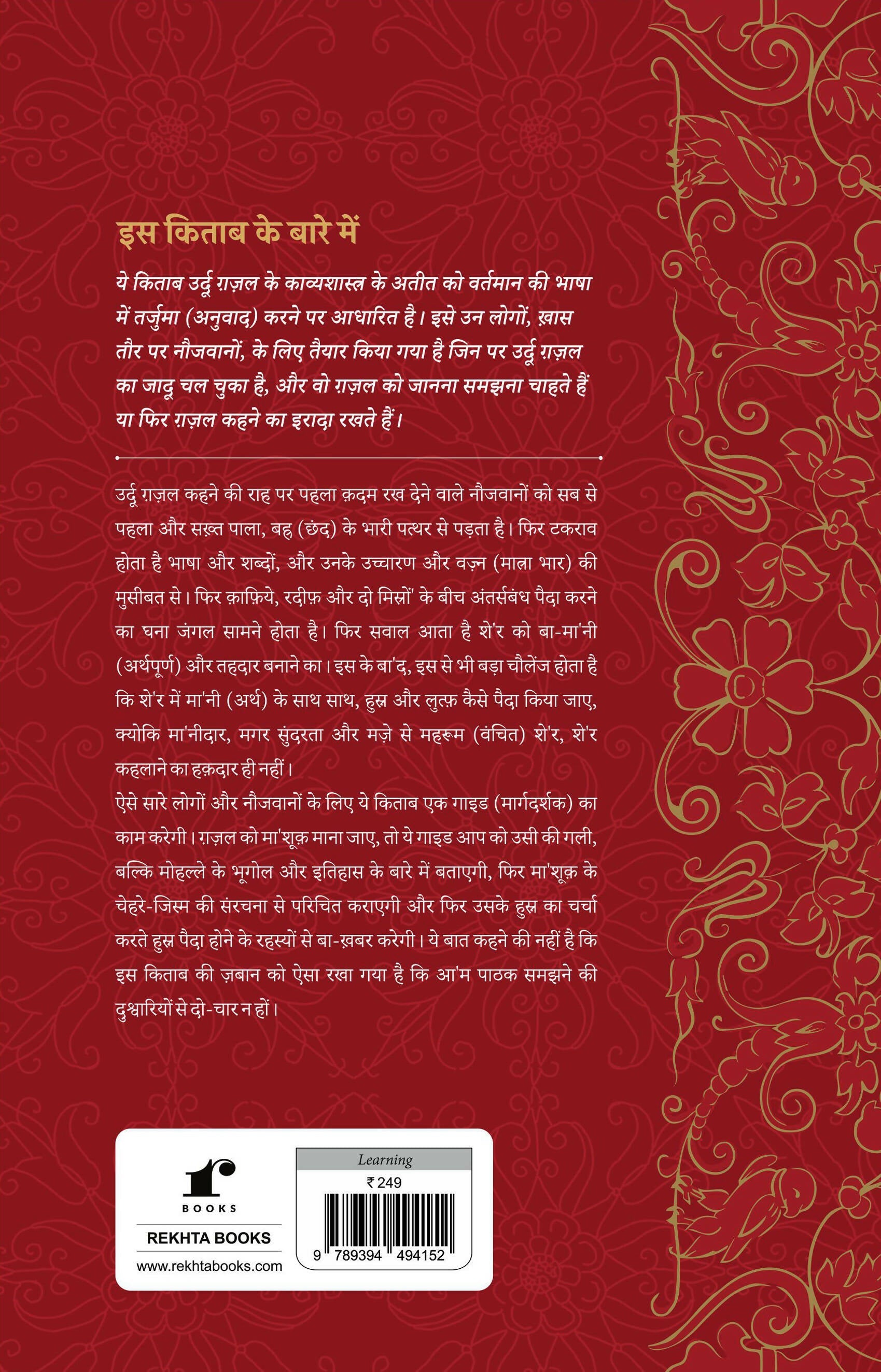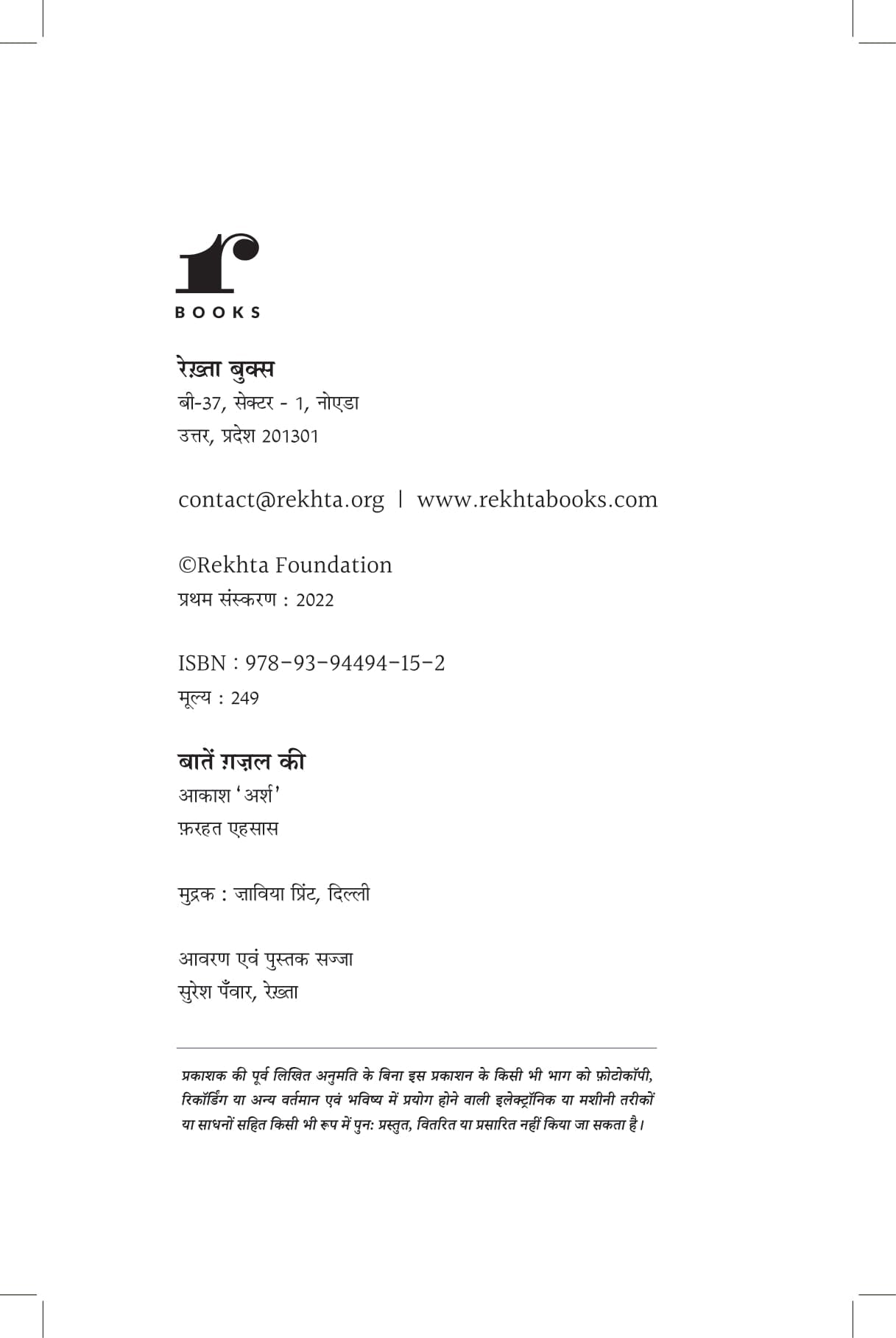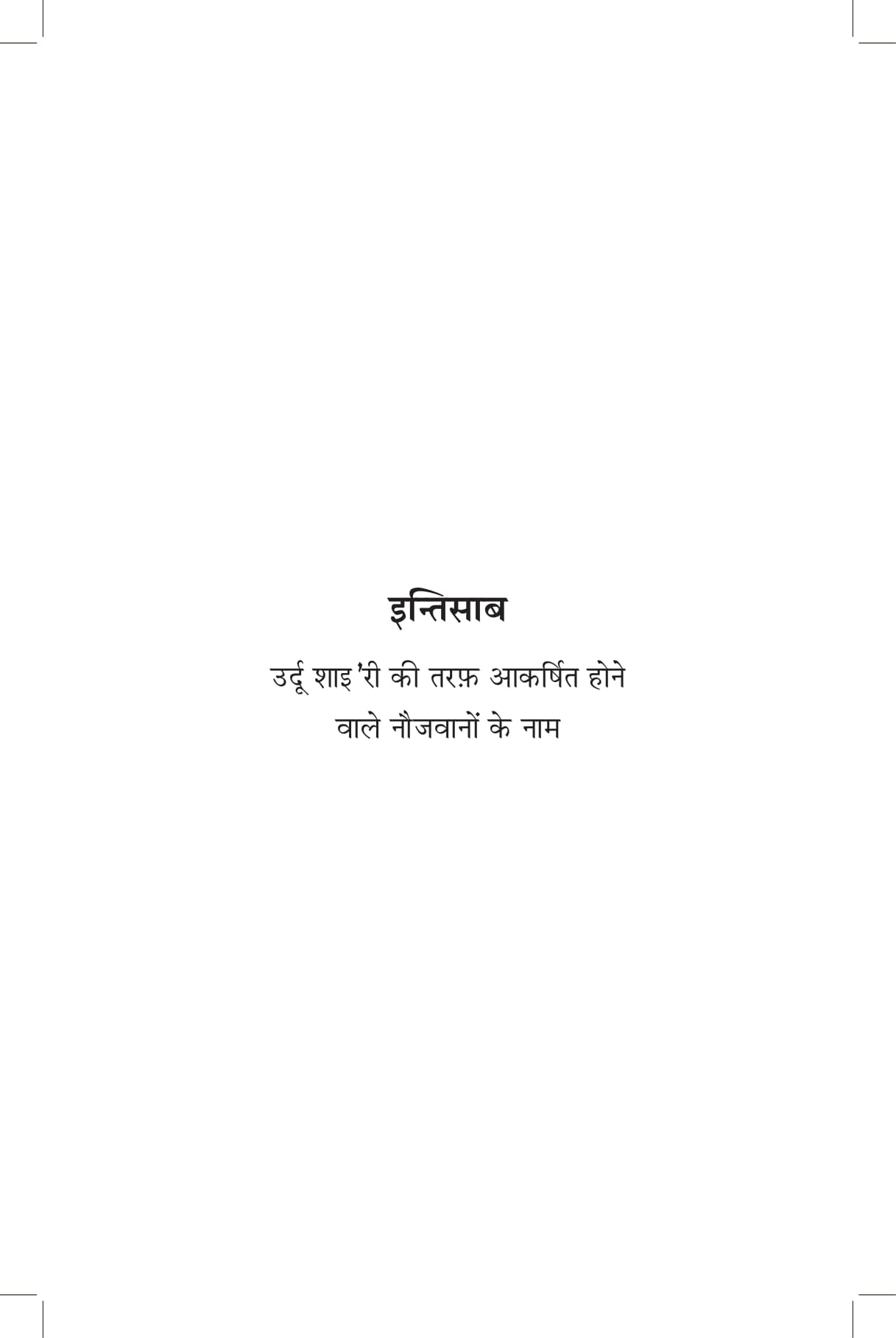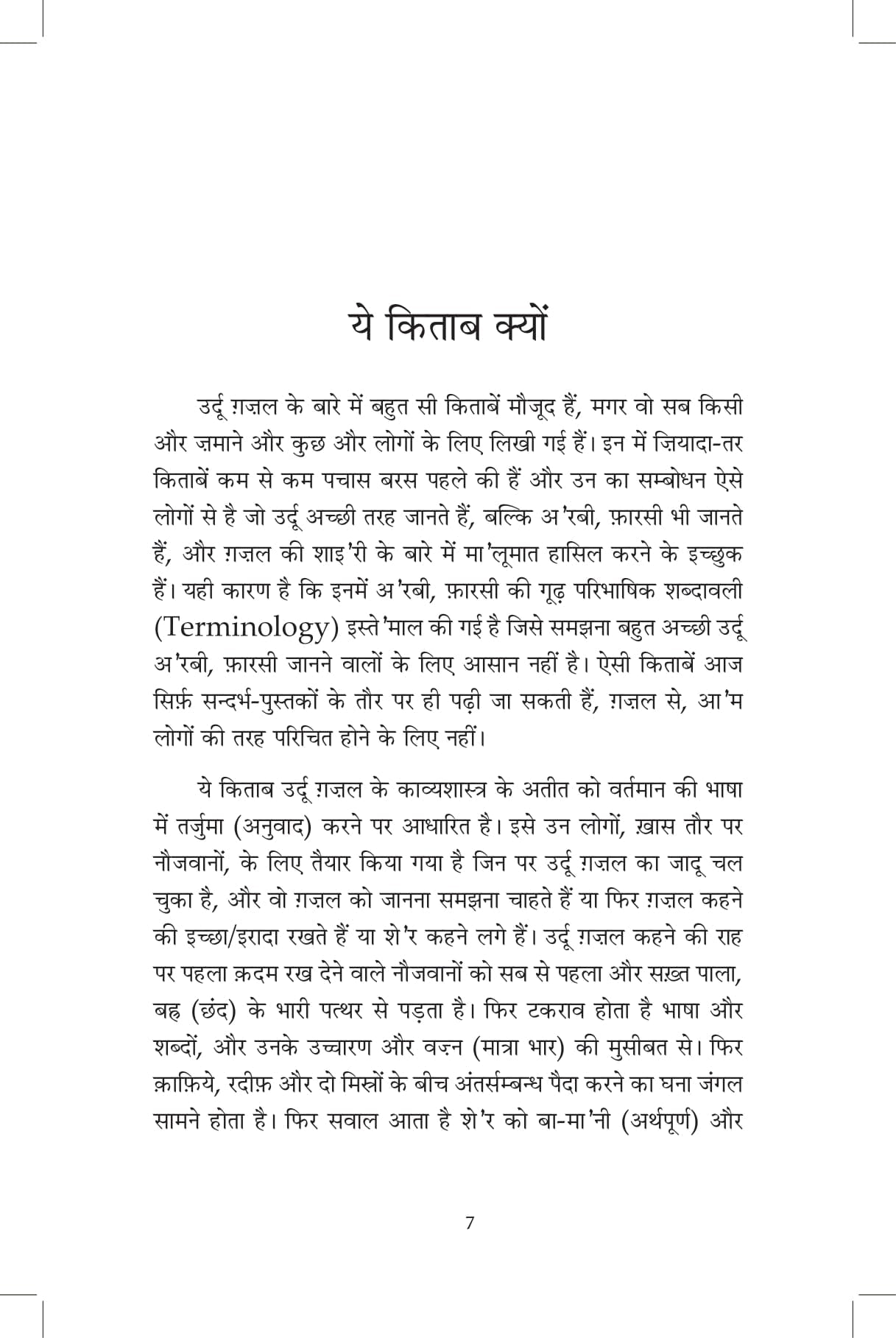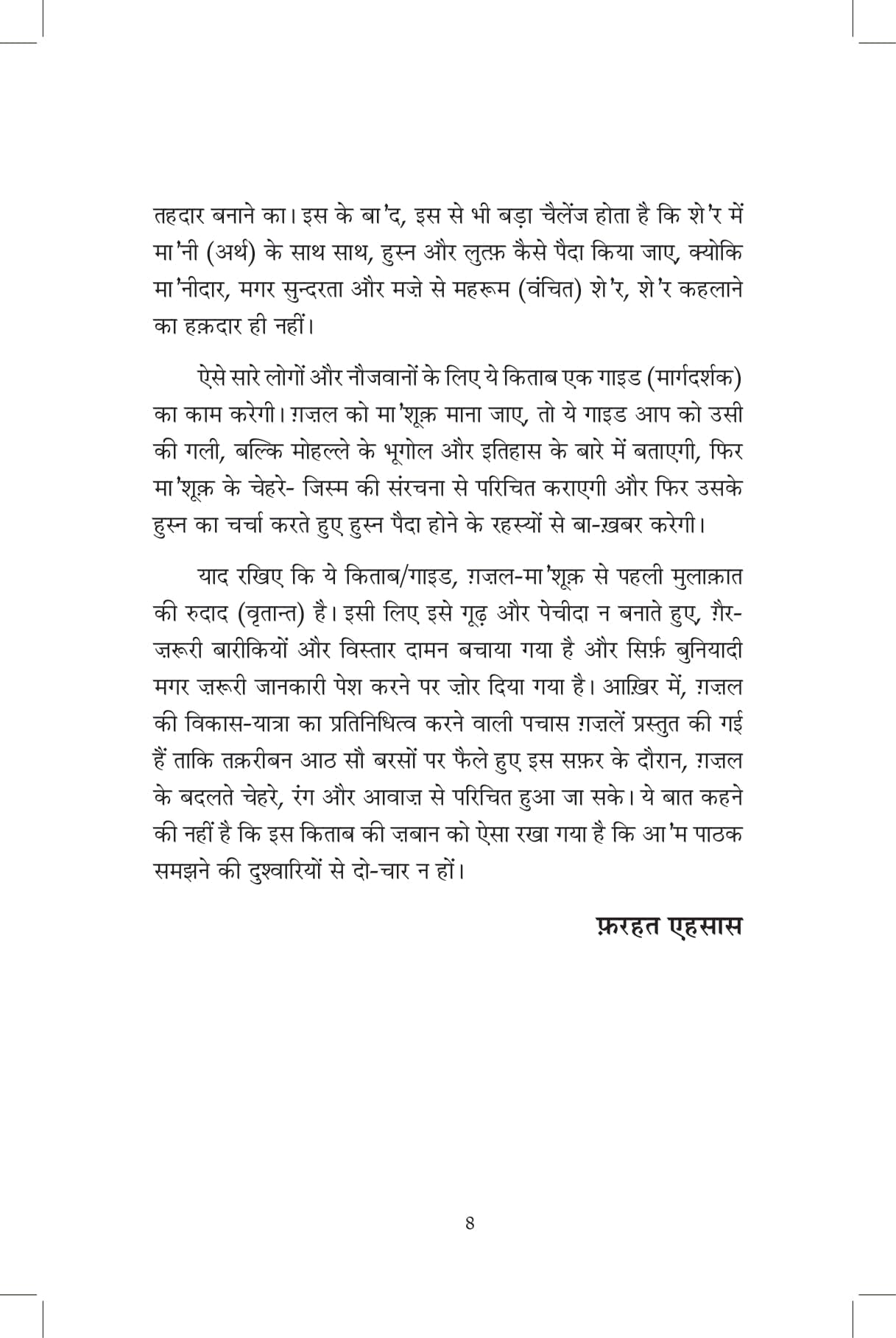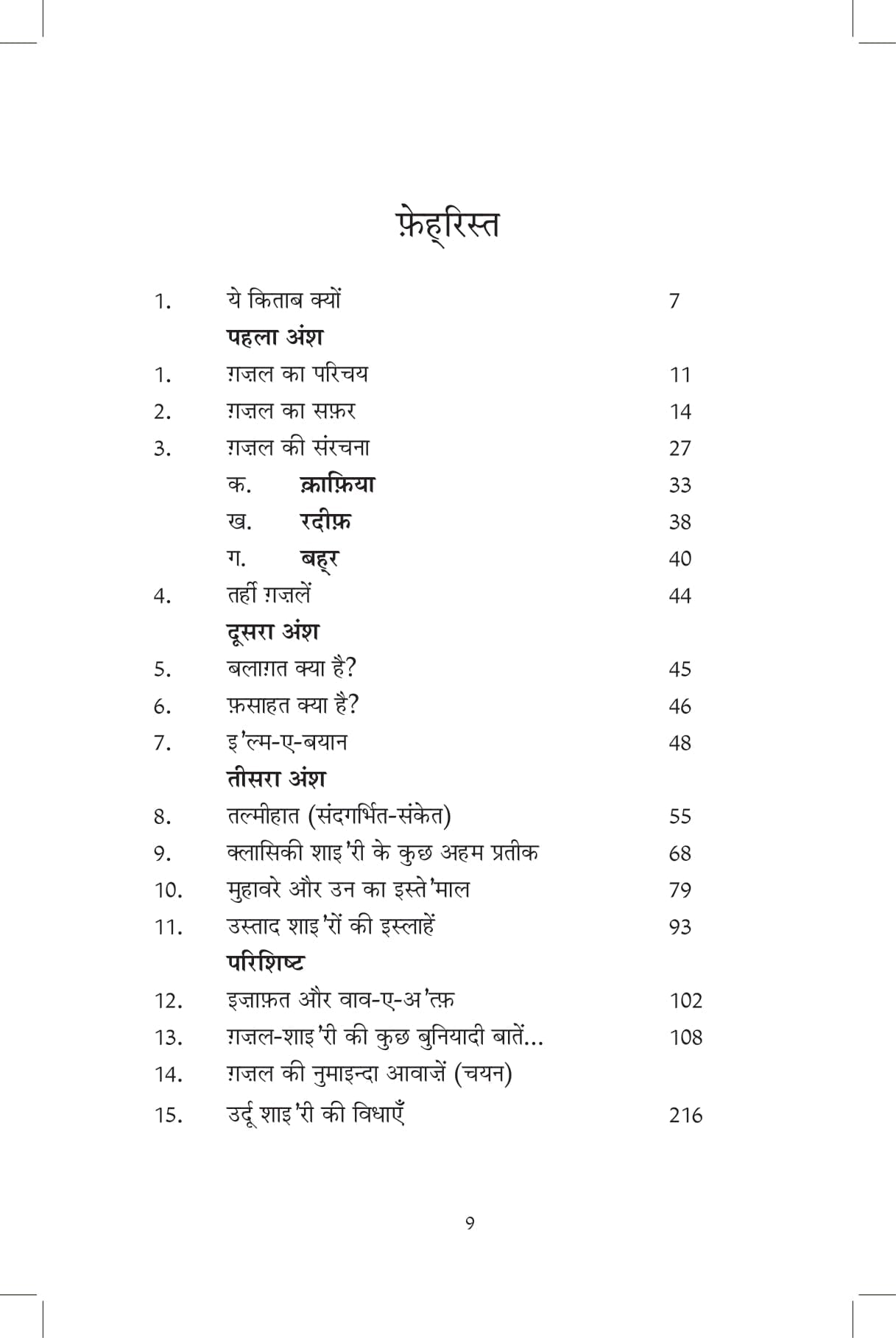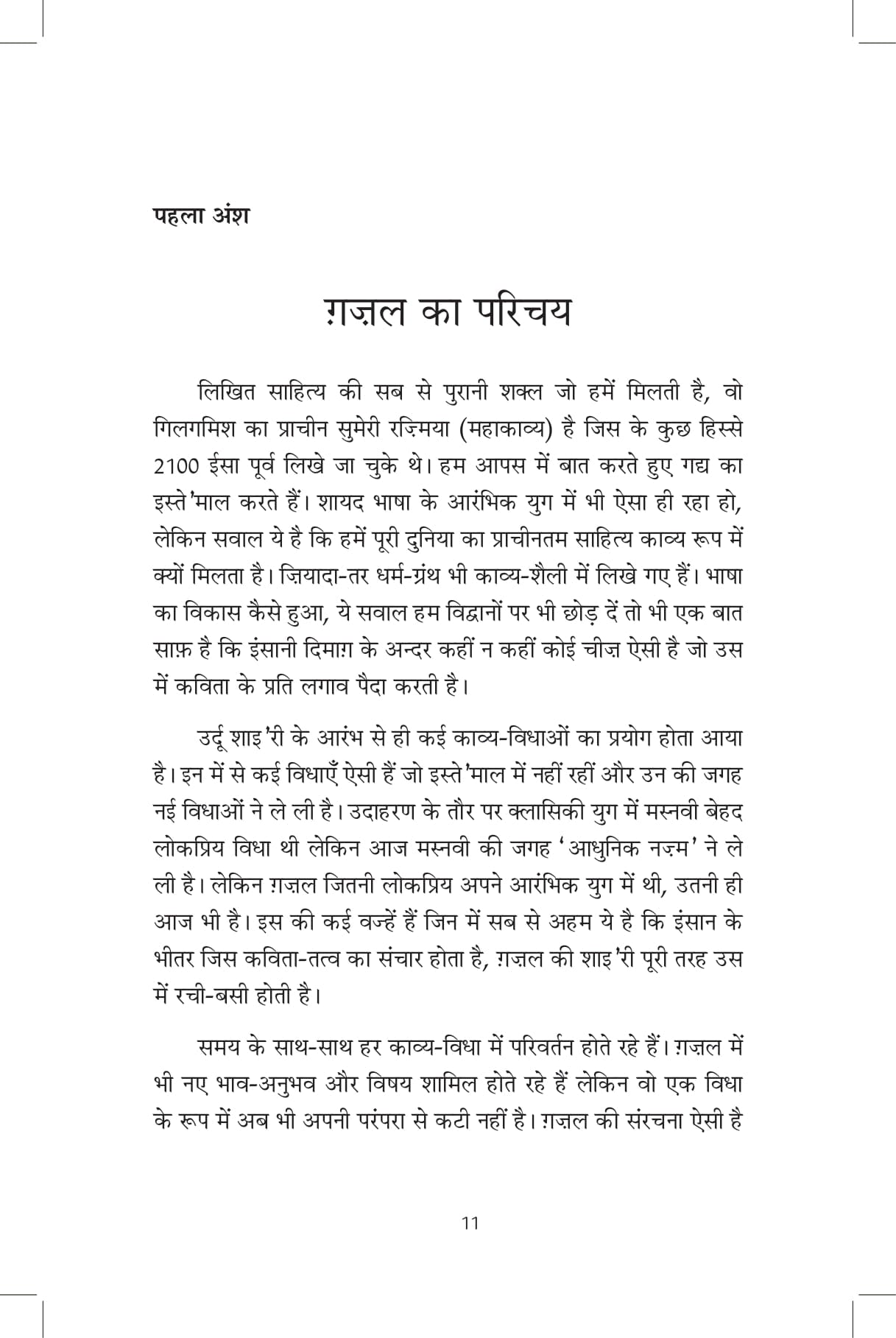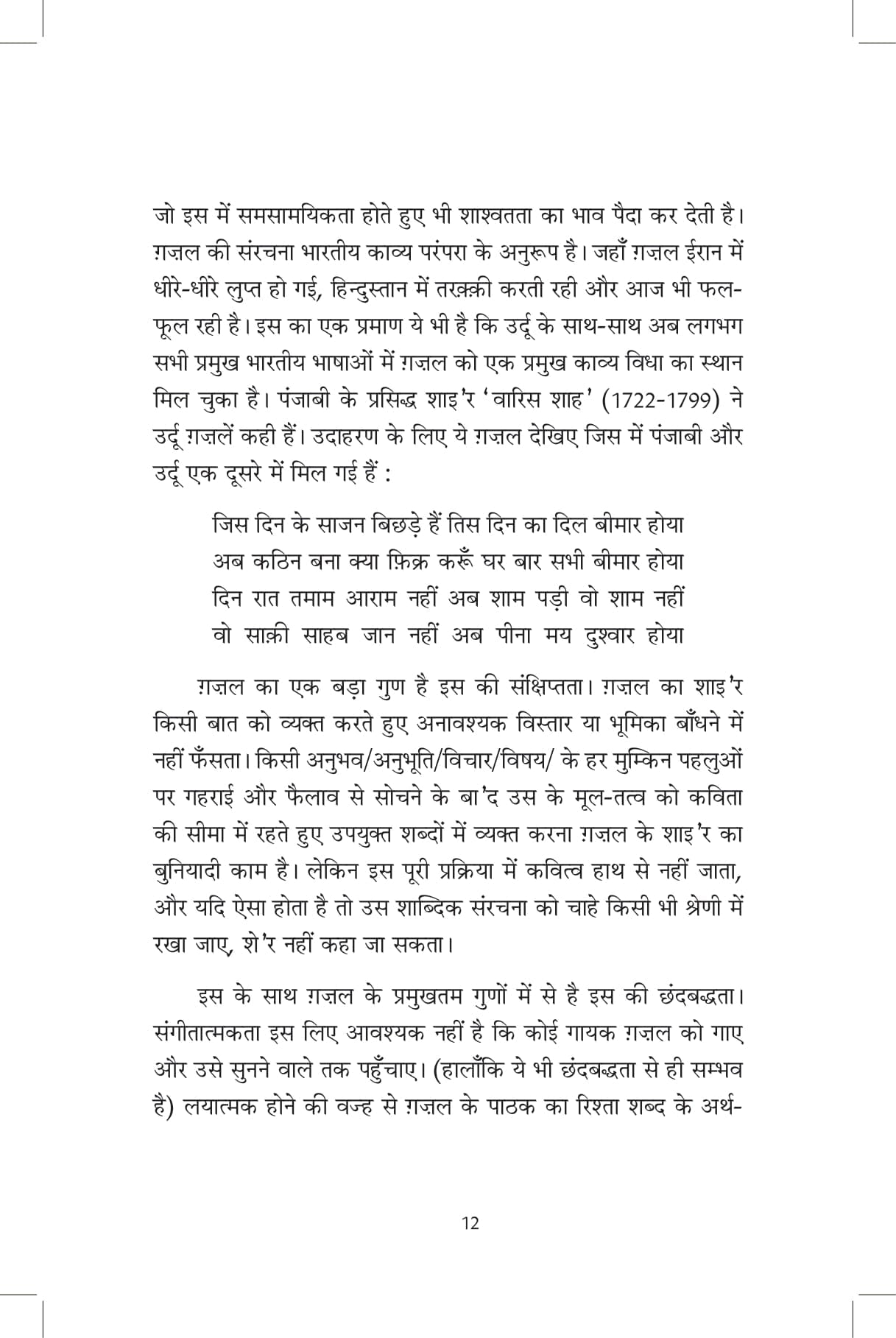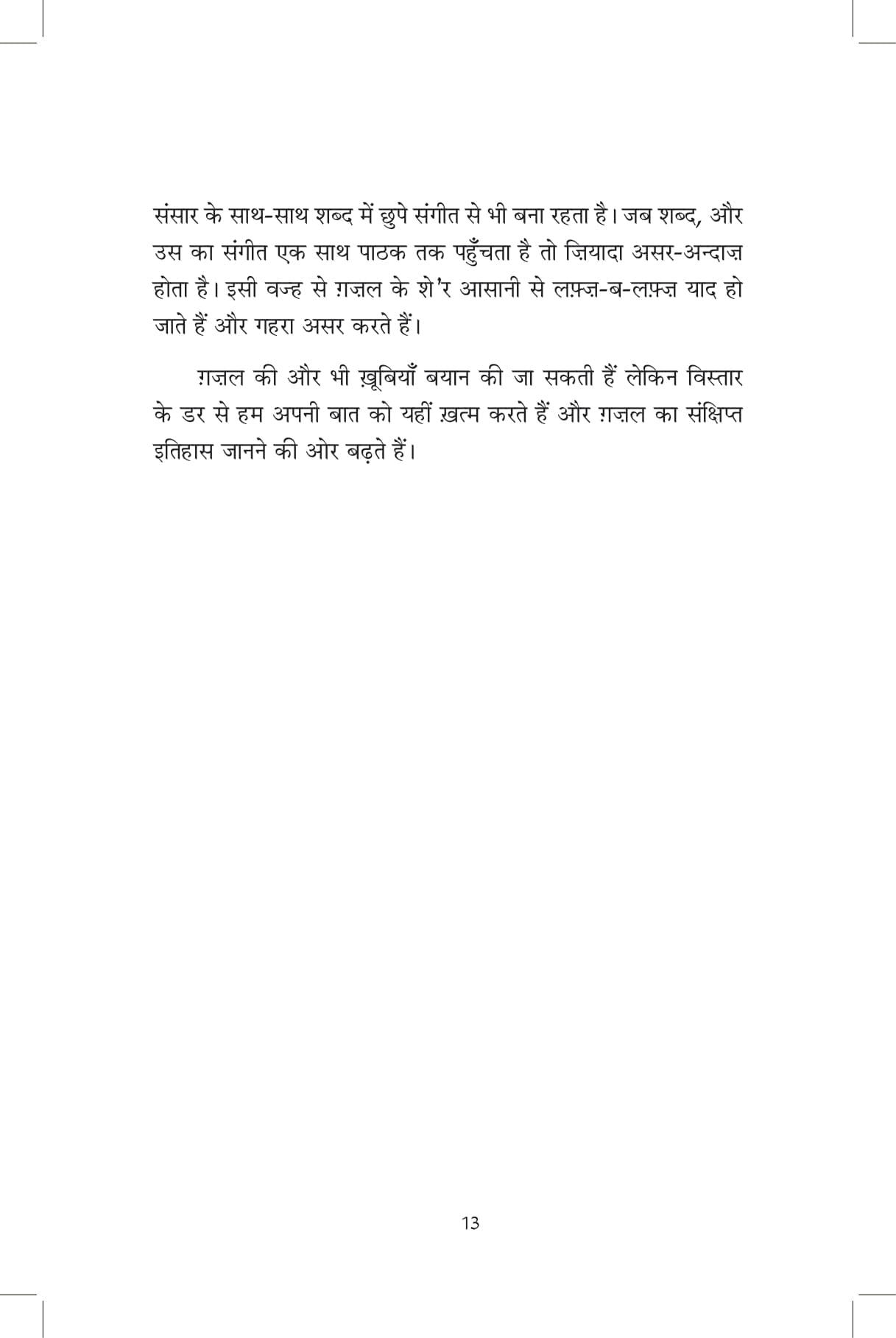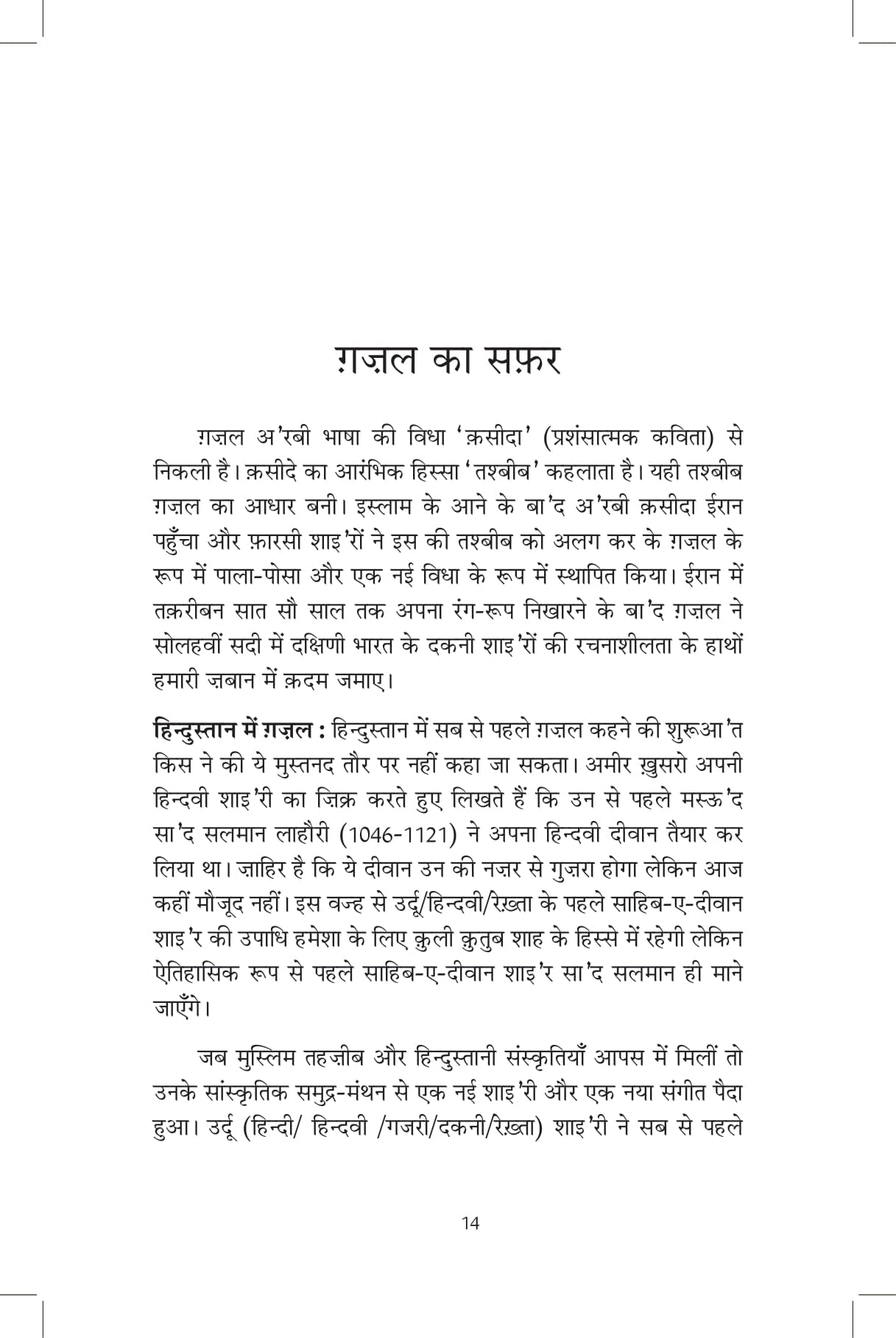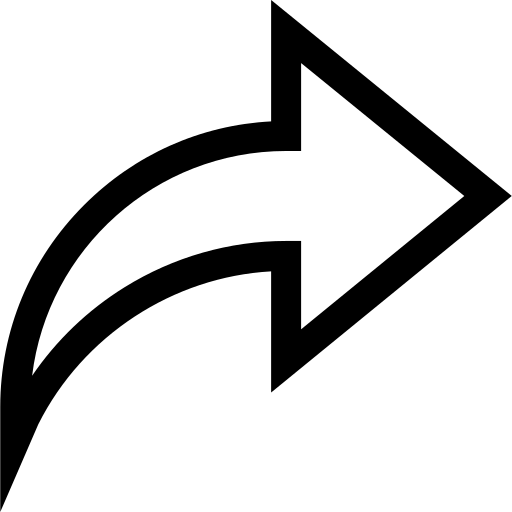Baatein Ghazal Ki
| Author | Farhat Ehsas, Arsh Sultanpuri |
| Language | Hindi |
| Publisher | Rekhta Publications |
| Pages | 219 |
| ISBN | 978-9394494152 |
| Book Type | Paperback |
| Item Weight | 0.4 kg |
| Edition | 1st |
| Series | 1st |
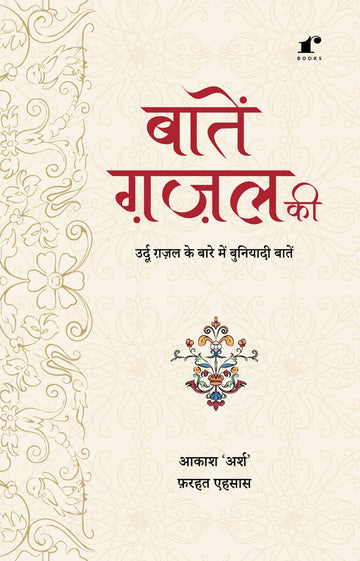
Baatein Ghazal Ki
About The Book:- The world of Urdu Ghazal is an enchanting and magnificent one. Many poetry enthusiasts are attracted to this genre of poetry, but can’t find a source to help them understand Ghazal's fundamental and foundational concepts. This book is specially intended for such readers. The book discusses the history of the Urdu Ghazal, The structural nuances of the Ghazal, and its poetics. Also, a selection of 50 Ghazals with commentary is included at the end for readers.
उर्दू ग़ज़ल की दुनिया विस्मयकारी है। कई काव्यप्रेमी काव्य की इस विधा की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उन्हें ग़ज़ल की मौलिक और मूलभूत अवधारणाओं को समझने में के लिए कोई अच्छा स्रोत नहीं मिलता। यह पुस्तक विशेष रूप से ऐसे पाठकों के लिए है जो ग़ज़ल की मूलभूत अवधारणाओं और काव्य-मूल्यों को समझना चाहते हैं। पुस्तक में उर्दू ग़ज़ल के इतिहास, ग़ज़ल की संरचनात्मक बारीकियों और इस के काव्यशास्त्र पर चर्चा की गई है। साथ ही, पाठकों के लिए अंत में 50 ग़ज़लों का टिप्पनी-सहित चयन भी शामिल किया गया है।
About the Authors:- आकाश ‘अर्श (आकाश तिवारी) सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 मई 2001 को पैदा हुए। प्रारम्भिक शिक्षा जगराओं, पंजाब में पूरी की। चार भाषाओं - उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी के साहित्य में समान रूप से रुचि। उर्दू और पंजाबी भाषा में काव्य-सृजन। सक्रिय रूप से अनुवाद और संकलन कार्यों में लगे हुए हैं। रेख़्ता फ़ाउंडेशन में एडिटोरियल इग्ज़ेक्युटिव के पद पर कार्यरत।
फ़रहत एहसास (फ़रहतुल्लाह ख़ाँ) बहराइच (उत्तर प्रदेश) में 25 दिसम्बर 1950 को पैदा हुए। अ’लीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के बाद 1979 में दिल्ली से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक ‘हुजूम’ का सह-संपादन। 1987 में उर्दू दैनिक ‘क़ौमी आवाज़’ दिल्ली से जुड़े और कई वर्षों तक उस के इतवार एडीशन का संपादन किया जिस से उर्दू में रचनात्मक और वैचारिक पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित हुए। 1998 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जुड़े और वहाँ से प्रकाशित दो शोध-पत्रिकाओं (उर्दू, अंग्रेज़ी) के सह-संपादक के तौर पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और बी.बी.सी. उर्दू सर्विस के लिए कार्य किया और समसामयिक विषयों पर वार्ताएँ और टिप्पणियाँ प्रसारित कीं। फ़रहत एहसास अपने वैचारिक फैलाव और अनुभवों की विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। उर्दू के अलावा, हिंदी, ब्रज, अवधी और अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी व अन्य पश्चिमी भाषाओं के साहित्य के साथ गहरी दिलचस्पी। भारतीय और पश्चिमी दर्शन से भी अंतरंग वैचारिक संबंध। सम्प्रति रेख़्ता फ़ाउंडेशन में मुख्य संपादक के पद पर कार्यरत।
- Sabr– Your order is usually dispatched within 24 hours of placing the order.
- Raftaar– We offer express delivery, typically arriving in 2-5 days. Please keep your phone reachable.
- Sukoon– Easy returns and replacements within 7 days.
- Dastoor– COD and shipping charges may apply to certain items.
Use code FIRSTORDER to get 10% off your first order.
Use code REKHTA10 to get a discount of 10% on your next Order.
You can also Earn up to 20% Cashback with POP Coins and redeem it in your future orders.