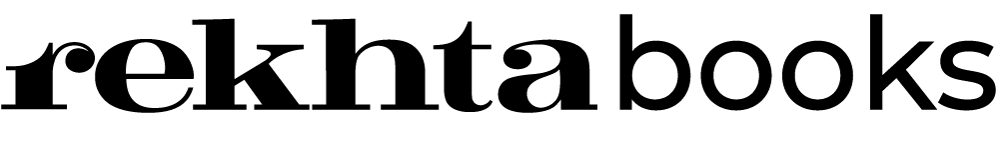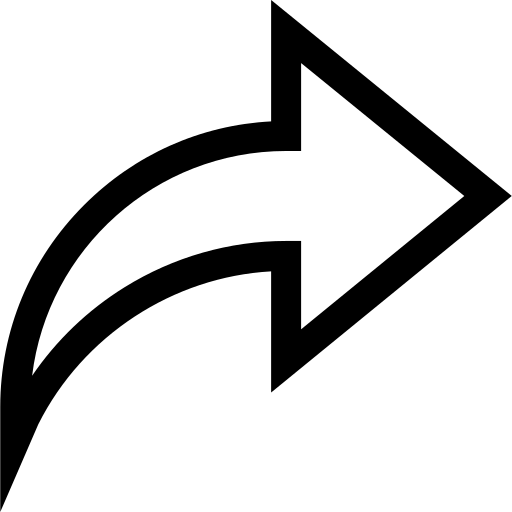Unke Andhkar mein Ujas hai
| ISBN | 978-93-91925-59-8 |
| Author | Sanjeev Buxy |
| Language | Hindi |
| Publisher | Antika Prakashan Pvt. Ltd. |
| Categories | Collection of Hindi Poems |
| Pages | 96 |
| Publishing year | 2023 |
| Return Policy | 5 days Return and Exchange |

Unke Andhkar mein Ujas hai
संजीव बख्शी की कविताओं में धरती पर पहली बारिश से उठी गंध जैसी ताजगी और सहजता महसूस होती है। उनकी दृष्टि और सरोकारों में सर्वत्र एक आदिवासी निश्चलता की व्याप्ति है। भाषा और शिल्प यानी संरचना और बिंब रचने जैसा कोई विशेष उपक्रम उनके यहाँ दिखाई नहीं देता। जो भी है वह स्वस्फूर्त है। धूल मिट्टी में सना होने के बावजूद अलौकिक आभा से दीप्त है। यह आभा उनके मानवीय सरोकारों और मनुष्यता में उनकी गहरी आस्था से उन्हें मिली है। काम से थके हुए मजदूर कुछ देर विश्राम के बाद उठते हैं और काम पर लग जाते हैं। श्रमिकों के इस दृश्य को देखिए। 'यहाँ जो सोए है विश्वकर्मा हैं देखना जागते ही पहुँच जाएँगे अपने अपने काम पर कोई गारा बनाने तो कोई दीवार कोई प्लास्टर कोई फर्श तो कोई छड़ काटेगा तो कोई ढोएगा रेत उनकी बातों का रस दीवार में शामिल हो जाएगा।' यह कैसे? ध्यान दीजिए कोई $खुश, कोई प्रकृतिस्थ कारीगर या कलाकार कभी अपने काम में त्रुटि नहीं छोड़ता। संजीव बख्शी की पक्षधरता मज़दूरों के साथ है। वे उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। संजीव बख्शी की कविता अधिक मार्मिक इसलिए है क्योंकि यह टूटे हुए फूलों के बलिदान के बारे में सोचती है। हम कोई भी दृश्य देखते हैं तो उसकी आवाज़ें भी सुनते हैं। इन कविताओं में जीवन की आवाज़ों का एक कठिन शास्त्रीय संगीत बजता है। दिन भर की व्यस्तता में काम की आवाज़ें, रेल की सीटी, कुकर की सीटी, पानी भरने का घमासान, स्कूल की बस और झुग्गी में रहने वाली बकरियाँ। सब शामिल इस जीवन राग में। संग्रह में ऐसी कई कविताएँ हैं जो उनकी कल्पनाशीलता और यथार्थ को पकडऩे की उत्सुकता का प्रमाण देती है। निश्चय की उन्हें आगे जाना है। और वे जाएँगे। —नरेश सक्सेना
About Author
Renowned Writer
- Sabr– Your order is usually dispatched within 24 hours of placing the order.
- Raftaar– We offer express delivery, typically arriving in 2-5 days. Please keep your phone reachable.
- Sukoon– Easy returns and replacements within 5 days.
- Dastoor– COD and shipping charges may apply to certain items.
Use code FIRSTORDER to get 5% off your first order.
You can also Earn up to 10% Cashback with POP Coins and redeem it in your future orders.