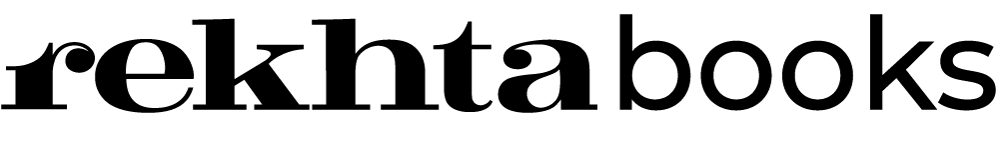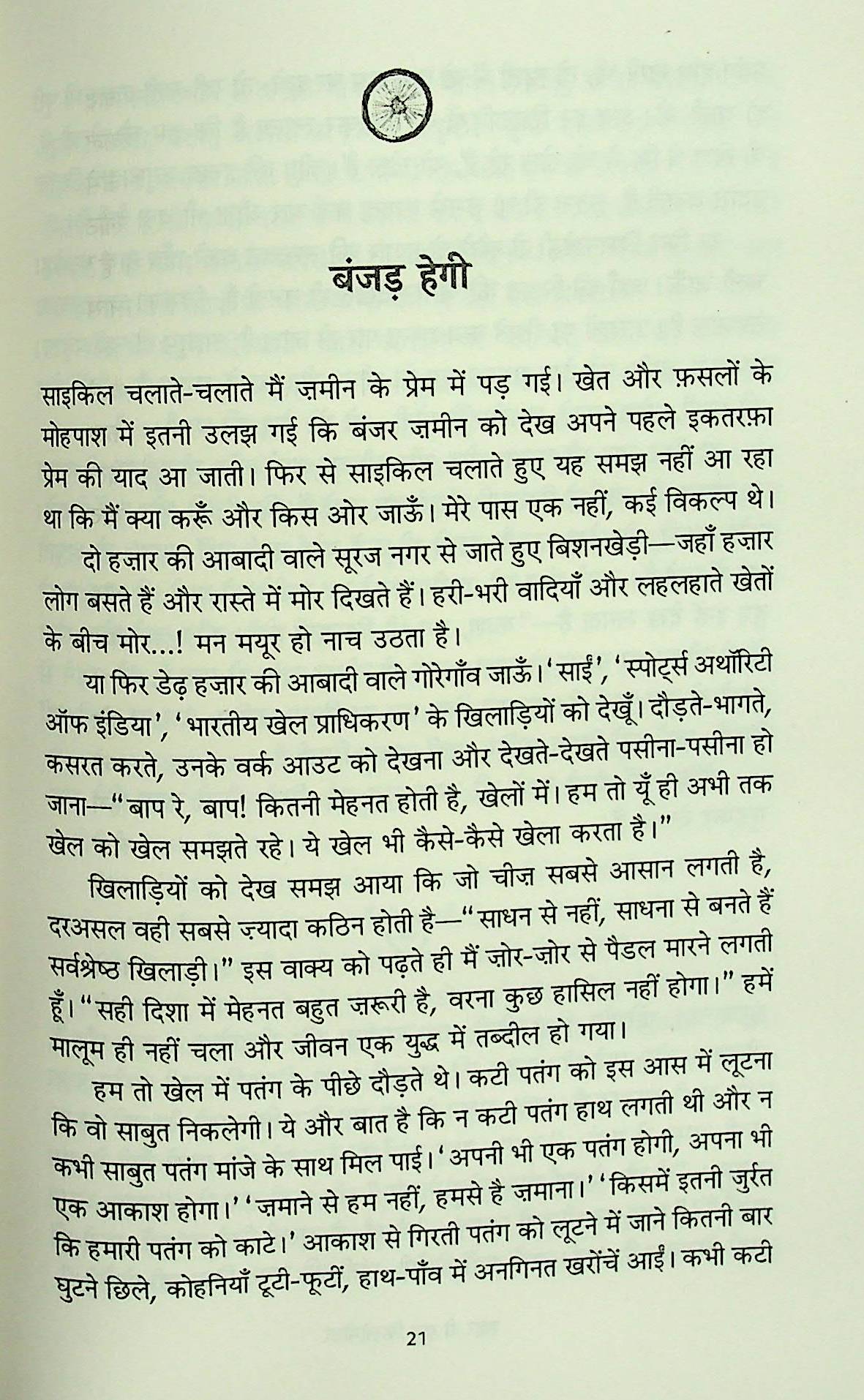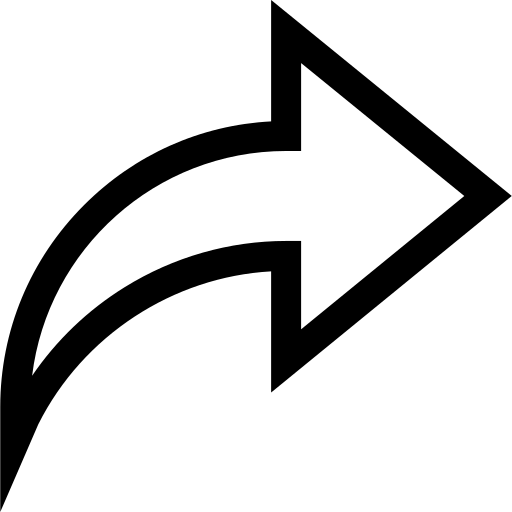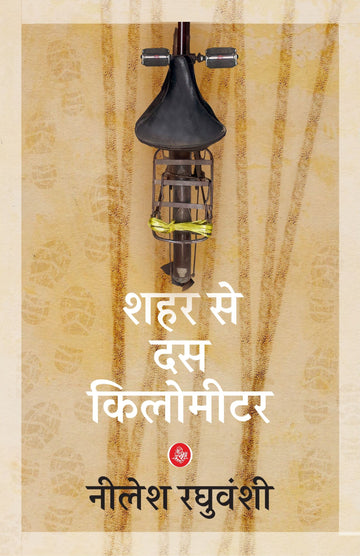बंजड़ हेगी
साइकिल चलाते-चलाते मैं ज़मीन के प्रेम में पड़ गई। खेत और फ़सलों के
मोहपाश में इतनी उलझ गई कि बंजर ज़मीन को देख अपने पहले इकतरफ़ा
प्रेम की याद आ जाती। फिर से साइकिल चलाते हुए यह समझ नहीं आ रहा
था कि मैं क्या करूँ और किस ओर जाऊँ। मेरे पास एक नहीं, कई विकल्प थे।
दो हज़ार की आबादी वाले सूरज नगर से जाते हुए बिशनखेड़ी—जहाँ हज़ार
लोग बसते हैं और रास्ते में मोर दिखते हैं । हरी-भरी वादियाँ और लहलहाते खेतों
के बीच मोर...! मन मयूर हो नाच उठता है ।
या फिर डेढ़ हज़ार की आबादी वाले गोरेगाँव जाऊँ । 'साईं', 'स्पोर्ट्स अथॉरिटी
ऑफ इंडिया', ‘भारतीय खेल प्राधिकरण' के खिलाड़ियों को देखूँ । दौड़ते-भागते,
कसरत करते, उनके वर्क आउट को देखना और देखते-देखते पसीना-पसीना हो
जाना—“बाप रे, बाप! कितनी मेहनत होती है, खेलों में। हम तो यूँ ही अभी तक
खेल को खेल समझते रहे। ये खेल भी कैसे-कैसे खेला करता है। "
खिलाड़ियों को देख समझ आया कि जो चीज़ सबसे आसान लगती है,
दरअसल वही सबसे ज़्यादा कठिन होती है—“ साधन से नहीं, साधना से बनते हैं
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी।” इस वाक्य को पढते ही मैं ज़ोर-ज़ोर से पैडल मारने लगती
हूँ। “सही दिशा में मेहनत बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ हासिल नहीं होगा।" हमें
मालूम ही नहीं चला और जीवन एक युद्ध में तब्दील हो गया। कभी
हम तो खेल में पतंग के पीछे दौड़ते थे। कटी पतंग को इस आस में लूटना
कि वो साबुत निकलेगी। ये और बात है कि न कटी पतंग हाथ लगती थी और न
साबुत पतंग मांजे के साथ मिल पाई। 'अपनी भी एक पतंग होगी, अपना भी
एक आकाश होगा।'' ज़माने से हम नहीं, हमसे है ज़माना ।' 'किसमें इतनी जुर्रत
कि हमारी पतंग को काटे।' आकाश से गिरती पतंग को लूटने में जाने कितनी बार
घुटने छिले, कोहनियाँ टूटी-फूटी, हाथ-पाँव में अनगिनत खरोंचें आईं। कभी कटी
ज़हरीले जीव पेड़ पर सरसराएँगे, तो जान हलक़ में फँस जाएगी।
लेकिन, दादा को मचान ज़रूर बनाना चाहिए।
दूसरे दिन मचान के नाम पर दद्दू बिफर गए । वे दूर खेत के उस पार अपनी
गायों और बछिया को चरा रहे थे। अम्मा ने उन्हें आवाज़ दी - 'हो' । वो कुछ
थकी और उलझी हुई सी थी ।
"अम्मा, आज सवेरे-सवेरे ? " मचान को मन में दबाए मैंने पूछा।
"अरे, दोपहर होने को आई । सवेरा तो कब का हो गया और चलो भी
गओ। हम तो सबरी रात से पहरेदारी कर रहे हैं । जे ढोरों ने नाक में दम कर
रखी है। देखो, जे देखो, आधो मक्का सफाचट कर गए कछु समझ नहीं आ
रही का करें? थोड़े भुट्टा लड़कियाँ तोड़ के घर लाई । मनो, वे तो मौं में धरते
ही जैसे दूध छोड़ रहे हैं। भुट्टा पके ई नहीं हैं अभी । ढोर-बछेडू प्राण ले लेंऐ
अबकी दफा तो।"
“ये ढोर-बछेड़ आते कहाँ से हैं। आवारा हैं क्या? कौन के हैं?"
"अरे, जहीं के नासपीटों के हैं। जलकुकड़ों के, कामचोरों के। दिन भर बाँध
के रखतें और रात में छोड़ देते हैं। उनसे गरीबन की फसल देखी नईं जात है।
पूरे तार काट दए इन लोगों ने। आधी रात को घुसेड़ देत हैं, जे अपने बछेडू । "
वो उनको जमकर ललकार रही थी। ये और बात है कि वो अभी आसपास
कहीं नहीं थे।
'अम्मा, मचान बना लो। पूरे खेत की रखवाली हो जाएगी।" मन की बात
बाहर आ ही गई।
"अरे, मचान से का हो जाएगो? मचान पे ठाड़े-ठाड़े थोड़ी न ढोर- बछेडू
भग जाएँगे। कौन अपने हैं कि 'हूका' देवे से हट जाएँगे। तुमरे दादा अकेले
कब तक दौड़ेंगे और दूसरे जीव-जन्तु भी रात में टहलते हैं। अब पहले जैसी
बात नहीं रही कि मचान पर चढ़ गए।"
'अम्मा, एक छोर पे दादा, दूसरे पर बेटा और तुम मचान पर। नंदू को
कहो न, फसल पीक पर है तो कुछ दिन देख ले।”
वो बारिश से पहले की सुबह नहीं थी । पानी गिरने में अभी समय था। अभी
समय था कि पूरा नीलबड़ पानी में तर हो जाए । सूनी-सपाट सड़कों को चमकने
में अभी देर थी। अभी देर थी कि पानी से बचतीं गायें यहाँ-वहाँ बेचैनी में रास्ता
पार करती दिखें। गाय गीले में नहीं बैठती। उसे गीलेपन से भयानक परहेज है।
वो बारिश में ख़ुद को बचाते नीचा सिर किए सूखी जगह ढूँढ़ती फिरती हैं। यह
सब होने में अभी समय था कि दो औरतें सड़क पर छतरी लिये बतियाती चली
आ रही हैं। थोड़े से अन्तराल के बाद फिर दो, फिर चार, फिर छह । छतरी लिये
औरतों से सड़क ख़ुशनुमा हो रही थी ।
छतरी लिये वे सब बहुत ख़ुश थीं ।
" छतरी तो बरसात के लिए होती है? "
"नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैडम कहती हैं कि तुम लोग इतनी कड़ी धूप
दिन भर खेत में काम करते हो, लू लग जाएगी। गरमी के लिए भी छतरी होती
है। बरसात में पानी से बचाती है तो गरमियों में घाम से बचाएगी। बहुत अच्छी
मैडम हैं वे। हर साल छतरी देती हैं हम लोगों को। कभी तो साल में दो बार भी
दे देती हैं। देतीं लेकिन सिर्फ औरतों को ही हैं । "
काकी को भी छतरी मिली। अब फार्म हाउस आते-जाते, सड़क पार करते,
पुलिया पर गपियाते, हर समय काकी छतरी के साथ ही दिखती है।
एक दिन भरी दुपहरी में टपरे में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी
की भी आहट नहीं। बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे थे। हर दिन चहल-पहल बनी
रहती थी, कभी कम, कभी ज़्यादा ।
कुछ दूर पर काकी नंगे पाँव चली जा रही है- " काकी चप्पलें कहाँ
चली गईं?"
"ससुर रीत गए हमारे। गाँव जा रही हूँ।”
"नंगे पाँव?"
"बूढ़े - सयानों की रीति है । हमरे जहाँ आदमी, औरतें सब नंगे पाँव रहें।
'अरे, लेकिन अकेली जा रही हो क्या? काका कहाँ हैं?'
“वे आगे निकल गए। बस स्टैंड के कना । वहीं मिल जेंऐ ।”
चटकती गरमी में खुले पार्क में अम्माजी ने सबको धौंस पिलाई - " किचिन में
पंखा लगवाओ, मैडम जी । हमको तुमरे एसी से कोई जलन-वलन नहीं है। मनो,
बाइयाँ भी इंसान हैं। करौरी लेकर घर थोड़ी न जाएँगी। अरे, पूरी पीठ भर जाती
है घमौरियों से। ना, अगली गर्मी नहीं। अभी तुरत व्यवस्था करवाओ। हमको
कोई पावडर - वावडर नहीं चाहिए। "
तीज-त्योहारों, खासकर दीवाली पर बाइयाँ सारे घरों में दूसरों के दिए उपहार
दिखाती हैं। वे यह बताना भी नहीं भूलतीं कि फलाँ नम्बर वाली ने अपनी बाई को
पुरानी साड़ी में नई फॉल लगाकर दी, तो उसने ख़ूब खरी-खरी सुनाई और साड़ी
नहीं ली। कह दिया उसने साफ़-साफ़ - " मैडमजी आप ही रखो ये साड़ी । कहीं
और लेने-देने में काम आ जाएगी।" आँखें चौड़ी कर हाथ नचाते, फुसफुसाते
सब अपने-अपने काम-घरों में यह क़िस्सा सुनातीं—“दीदी, फलाँ नम्बर वाली
की भौत थू-थू हो रही है सब दूर। ऐसे करेगी, तो कोई बाई उसके यहाँ काम
नहीं करेगी।” सुनने वाली अपनी घबराहट को छिपाते हुए मन ही मन 'वो क्या
दे' या कि “जो सोचा था, उसे बदलकर कुछ और देना होगा। कहीं उसकी भी
'थू-थू' हो गई तो...।"
अम्माजी के नियम-क़ानून ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। हर घर के
कैलेंडर में बाई का खाता खुल गया। उसके चार दिन की छुट्टी का हिसाब
रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर कम है, तो पैसा देना है और अगर ज़्यादा
हैं तो काट लेना है। पूरे महीने बिल्ली-चूहे सी जंग छिड़ी रहती है। अगर किसी
के घर में दो बाई हैं और अगर एक ने छुट्टी ली, तो उसका काम दूसरी बाई ने
किया या आपने कराया, तो उसके पैसे का हिसाब भी रखना पड़ता है। छुट्टी
के गोले अलग और अतिरिक्त काम के गोले अलग से बनाए जाते हैं।
इन गोलों की डिजाइन और हिसाब में किसी तरह की चूक न हो। ये मुद्दा
हर किटी पार्टी में छाया रहता है। नई-नई तकनीक ईजाद की जाती हैं। कुछ
को इस हिसाब से बहुत चिढ़ मचती है, तो कुछ को परम आनन्द की प्राप्ति
मिलती है। भजन मंडली में बूढ़ी सयानी औरतें बाइयों की इस हेकड़ी और नए
तौर-तरीक़ों पर ठंडी साँसें भरते हुए कहती हैं—“हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं
शहर से दस किलोमीट