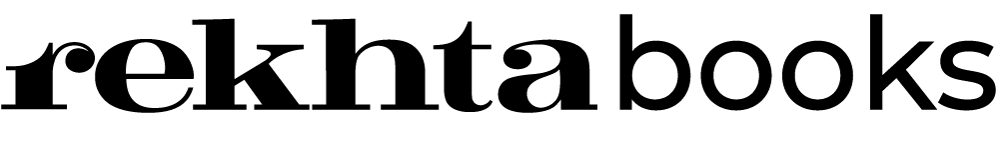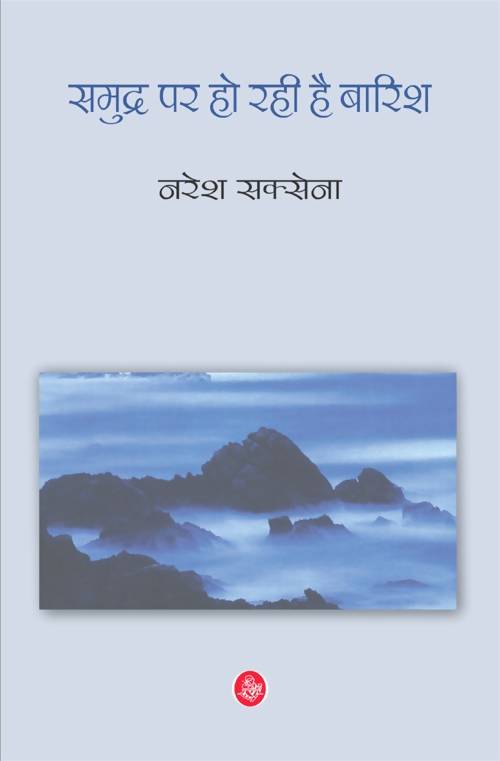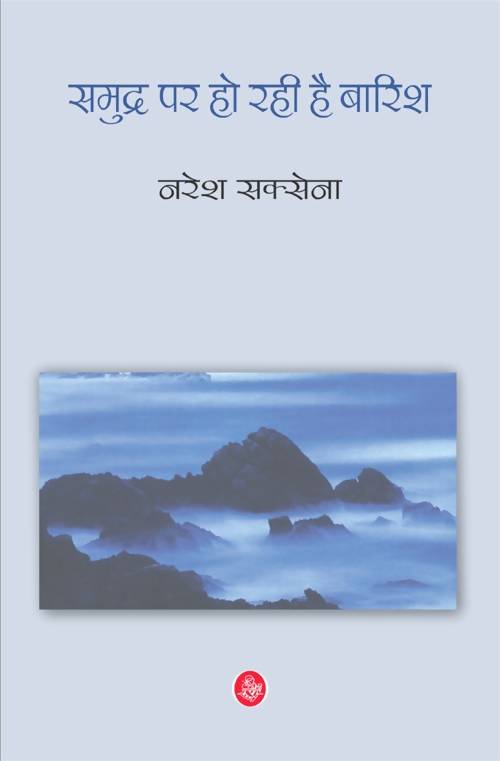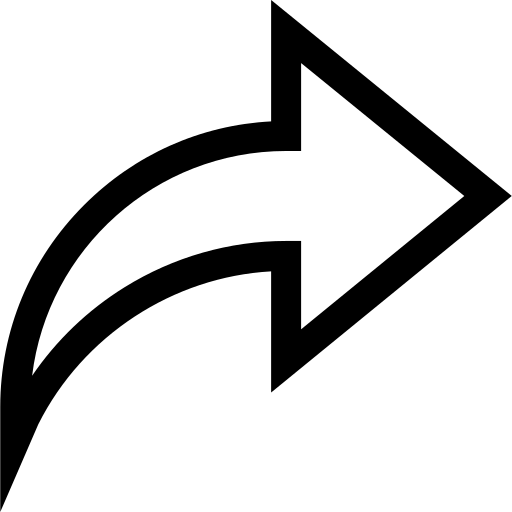Samundra Par Ho Rahi Hai Barish
| Item Weight | 500 Grams |
| ISBN | 978-8126702077 |
| Author | Naresh Saxena |
| Language | Hindi |
| Publisher | Rajkamal Prakashan |
| Pages | 94p |
| Dimensions | 26*16*7 |
| Publishing year | 0 |
| Edition | 3rd |
| Return Policy | 5 days Return and Exchange |
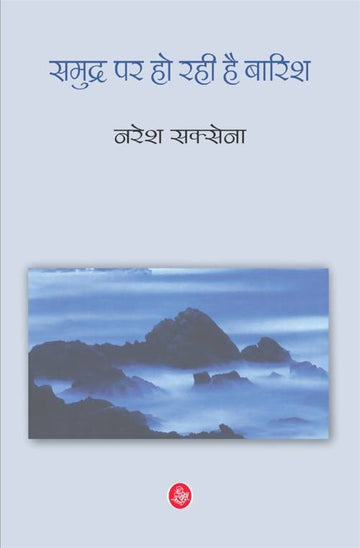
Samundra Par Ho Rahi Hai Barish
एक अद्वितीय तत्त्व हमें नरेश सक्सेना की कविता में दिखाई पड़ता है जो शायद समस्त भारतीय कविता में दुर्लभ है और वह है मानव और प्रकृति के बीच लगभग संपूर्ण तादात्म्य—और यहाँ प्रकृति से अभिप्राय किसी रूमानी, ऐंद्रिक शरण्य नहीं बल्कि पृथ्वी सहित सारे ब्रह्मांड से है, वे सारी वस्तुएँ हैं जिनसे मानव निर्मित होता है और वे भी जिन्हें वह निर्मित करता है। मुक्तिबोध के बाद की हिंदी कविता यदि ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ को नए अर्थों में अभिव्यक्त कर रही है तो उसके पीछे नरेश सरीखी प्रतिभा का योगदान अनन्य है। धरती को माता कह देना सुपरिचित है किंतु नरेश उसके अपनी धुरी पर घूमने के साथ-साथ प्रदक्षिणा करने तथा उसके शरीर के भीतर के ताप, आद्र्रता, दबाव, रत्नों और हीरों से रूपक रचते हुए उसे पहले पृथ्वी-स्त्री संबोधित करते हैं। वे यह मूलभूत पार्थिव तथ्य भी नहीं भूलते कि आदमी कुछ प्राथमिक तत्त्वों से बना है–मानव-शरीर की निर्मिति में जल, लोहा, पारा, चूना, कोयला सब लगते हैं। ‘पहचान’ सरीखी मार्मिक कविता में कवि फलों, फूलों और हरियाली में अपने अंतिम बार लौटने का चित्र खींचता है जो ‘पंचतत्त्वों में विलीन होने’ का ही एक पर्याय है। नरेश यह किसी अध्यात्म या आधिभौतिकी से नहीं लेते–वे शायद हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने अपने अर्जित वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय एवं प्रतिबद्ध सृजन-धर्म में ढाल लिया है और इस जटिल प्रक्रिया में उन्होंने न तो विज्ञान को सरलीकृत किया है और न कविता को गरिष्ठ बनाया है। यांत्रिकी उनका अध्यवसाय और व्यवसाय रही है और नरेश ने नवगीतकार के रूप में अपनी प्रारंभिक लोकप्रियता को तजते हुए धातु-युग की उस कठोर कविता को वरा, जिसके प्रमुख अवयव लोहा, क्राँकीट और मनुष्य-शक्ति हैं। एक दृष्टि से वे मुक्तिबोध के बाद शायद सबसे ठोस और घनत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाओं में खून, पसीना, नमक, ईंट, गारा बार-बार लौटते हैं। दूसरी ओर उनकी कविता में पर्यावरण की कोई सीमा नहीं है। वह भौतिक से होता हुआ सामाजिक और निजी विश्व को भी समेट लेता है। हिंदी कविता में पर्यावरण को लेकर इतनी सजगता और स्नेह बहुत कम कवियों के पास है। विज्ञान, तकनीकी, प्रकृति और पर्यावरण से गहरे सरोकारों के बावजूद नरेश सक्सेना की कविता कुछ अपूर्ण ही रहती यदि उसके केंद्र में असंदिग्ध मानव-प्रतिबद्धता, जिजीविषा और संघर्षशीलता न होतीं। वे ऐसी ईंटें चाहते हैं जिनकी रंगत हो सुर्ख / बोली में धातुओं की खनक / ऐसी कि सात ईंटें चुन लें तो जलतरंग बजने लगे और जो घर उनसे बने उसे जाना जाए थोड़े से प्रेम, थोड़े से त्याग और थोड़े से साहस के लिए, किन्तु वे यह भी जानते हैं कि उन्हें ढोने वाली मज़दूरिन और उसके परिवार के लिए वे ईंटें क्या-क्या हो सकती हैं। जब वे दावा करते हैं कि दुनिया के नमक और लोहे में हमारा भी हिस्सा है तो उन्हें यह जि़म्मेदारी भी याद आती है कि फिर दुनिया-भर में बहते हुए खून और पसीने में/हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। पत्थरों से लदे ट्रक में सोए या बेहोश पड़े आदमी को वे जानते हैं जिसने गिट्टियाँ नहीं अपनी हड्डियाँ तोड़ी हैं/और हिसाब गिट्टियों का भी नहीं पाया। उधर हिंदुत्ववादी फासिस्ट ताकतों द्वारा बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर उनकी छोटी-सी कविता–जो इस शर्मनाक कुकृत्य पर हिंदी की शायद सर्वश्रेष्ठ रचना है–अत्यंत साहस से दुहरी धर्र्मांधता पर प्रहार करती है : इतिहास के बहुत से भ्रमों में से/ एक यह भी है/ कि महमूद गज़नवी लौट गया था/लौटा नहीं था वह/यहीं था / सैकड़ों बरस बाद अचानक / वह प्रकट हुआ अयोध्या में/सोमनाथ में उसने किया था / अल्लाह का काम तमाम / इस बार उसका नारा था / जय श्री राम। टी.एस. एलिअट ने कहीं कुछ ऐसा कहा है कि जब कोई प्रतिभा या पुस्तक साहित्य की परंपरा में शामिल होती है तो अपना स्थान पाने की प्रक्रिया में वह उस पूरे सिलसिले के अनुक्रम को न्यूनाधिक बदलती है–वह पहले जैसा नहीं रह पाता–और ऐसे हर नए पदार्पण के बाद यह होता चलता है। नरेश सक्सेना के साथ जटिल समस्या यह है कि यद्यपि वे पिछले चार दशकों से पाठकों और श्रोताओं में सुविख्यात हैं और सारे अच्छे–विशेषत: युवा–कवि उन्हें बहुत चाहते हैं किंतु अपना पहला संग्रह वे हिंदी को उस उम्र में दे रहे हैं जब अधिकांश कवि (कई तो उससे भी कम आयु में) या तो चुक गए होते हैं या अपनी ही जुगाली करने पर विवश होते हैं। अब जबकि नरेश के कवि-कर्म की पहली, ठोस और मुकम्मिल क़िस्त हमें उपलब्ध है तो पता चलता है कि वे लंबी दौड़ के उस ताकतवर फेफड़ोंवाले किंतु विनम्र धावक की तरह अचानक एक वेग-विस्फोट में आगे आ गए हैं जिसके मैदान में बने रहने को अब तक कुछ रियायत, अभिभावकत्व, कुतूहल और किंचित् परिहास से देखा जा रहा था। उनकी जल की बूँद जैसी अमुखर रचनाधर्मिता ने आखिरकार हिंदी की शिलाओं पर अपना हस्ताक्षर छोड़ दिया है और काव्येतिहास के पुनरीक्षण को उसी तरह लाजि़मी बना डाला है जैसे हमारे देखते-देखते मुक्तिबोध और शमशेर ने बना दिया था। —विष्णु खरे
Title: Samundra Par Ho Rahi Hai Barish | समुंद्र पर हो रही है बारिश
Author: Naresh Saxena | नरेश सक्सेना
- Sabr– Your order is usually dispatched within 24 hours of placing the order.
- Raftaar– We offer express delivery, typically arriving in 2-5 days. Please keep your phone reachable.
- Sukoon– Easy returns and replacements within 5 days.
- Dastoor– COD and shipping charges may apply to certain items.
Use code FIRSTORDER to get 5% off your first order.
You can also Earn up to 10% Cashback with POP Coins and redeem it in your future orders.