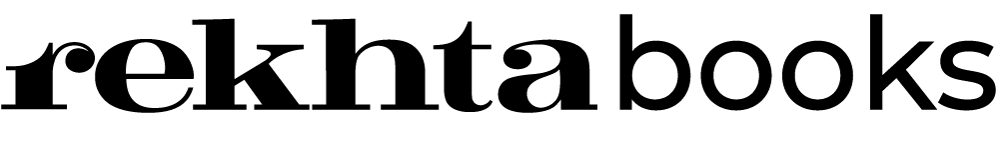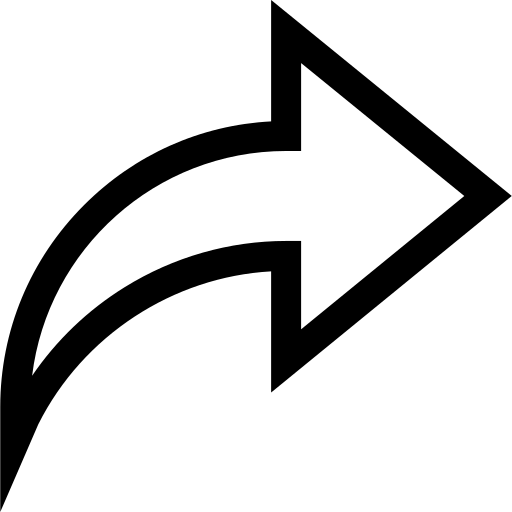Kya Raha Hai Mushayaron Mein Ab
Regular price
₹ 193
Sale price
₹ 193
Regular price
₹ 199
Unit price
Save 3%
| Author | Iqbal Rizvi |
| Publishing year | 0 |
| Return Policy | 5 days Return and Exchange |
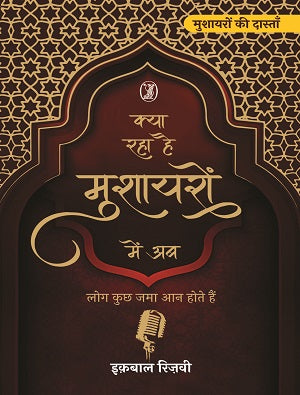
Kya Raha Hai Mushayaron Mein Ab
Product description
Shipping & Return
Offers & Coupons
भारतीय उपमहाद्वीप में मुशायरों और महफ़िलों की अपनी एक परम्परा और इतिहास रहा है। अपने मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए मुशायरे एक ऐसी जगह हुआ करते थे, जहाँ सुनने और सुनानेवाले दोनों एक-दूसरे के पूरक हुआ करते थे। मुशायरे का आरम्भ यूँ तो दरबारों और राजमहलों से माना जाता है लेकिन अरब जगत में मेलों के अवसर पर शायरों के जुटने का इतिहास भी मिलता है। अरबी और फ़ारसी के ज़रिये मुशायरे के आयोजन भारत पहुँचे, तो बरसों तक इसमें ख़ास लोग ही शामिल होते रहे। एक ज़माने में मुशायरे तहज़ीब के केन्द्र हुआ करते थे। आख़िरी मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र के लाल किले के मुशायरे अब इतिहास का हिस्सा हैं। इन मुशायरों में ग़ालिब सुनाते थे और जौक़ सुनते थे, बहादुर शाह ज़फ़र ग़ज़ल पढ़ते थे और सुननेवालों में मोमिन ख़ाँ, ग़ालिब, शेफ़्ता और युवा शायर दाग़ होते थे। उन दिनों सुनानेवालों और सुननेवालों के बीच में इतनी दूरी नहीं होती थी जितनी आज नज़र आती है। फिर जब उर्दू ने विस्तार पाया तो मुशायरों में कई वर्ग के लोग शामिल होने लगे। बाद में सामाजिक वातावरण और राज-व्यवस्था के बदलाव के साथ मुशायरों के तौर-तरीक़ों में भी बदलाव आने लगा। एक समय जो मुशायरे राजदरबारों, सामन्तों और अभिजात वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक हैसियत के पर्याय हुआ करते थे, धीरे-धीरे उन्होंने सार्वजनिक मंचों का रूप ले लिया। सार्वजनिक मंचों पर पढ़ी जानेवाली ग़ज़लों और नज़्मों की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि मुशायरों की तर्ज़ पर हिन्दी कविता भी कवि-सम्मेलनों में पढ़ी जाने लगी। दिल्ली के लाल किले पर हर वर्ष गणतन्त्र दिवस के मौके पर आयोजित होनेवाले मुशायरे और कवि-सम्मेलन तो लाल किला मुशायरा और लाल क़िला कवि-सम्मेलन के नाम से बेहद प्रसिद्ध हुआ करते थे। मुशायरों और कवि-सम्मेलनों की बढ़ती इस लोकप्रियता के चलते जहाँ श्रोताओं के स्वाद में परिवर्तन हुआ है, वहीं सत्ता का हस्तक्षेप भी बढ़ा है। इसलिए इन दोनों सार्वजनिक मंचों पर बेहतरीन शायरी या कविता पढ़ने को नहीं मिलती है बल्कि इनका स्थान चुटकलों और द्विअर्थी कविताओं ने ले लिया है। इक़बाल रिज़वी की यह पुस्तक मुशायरों के इसी अतीत और वर्तमान का विहंगावलोकन है। यह पुस्तक मुशायरों की उस गौरवशाली परम्परा को भी बयान करती है, जब इनमें सांस्कृतिक शालीनता और अदबी समझ की परख होती थी।
- Sabr– Your order is usually dispatched within 24 hours of placing the order.
- Raftaar– We offer express delivery, typically arriving in 2-5 days. Please keep your phone reachable.
- Sukoon– Easy returns and replacements within 5 days.
- Dastoor– COD and shipping charges may apply to certain items.
Use code FIRSTORDER to get 5% off your first order.
You can also Earn up to 10% Cashback with POP Coins and redeem it in your future orders.