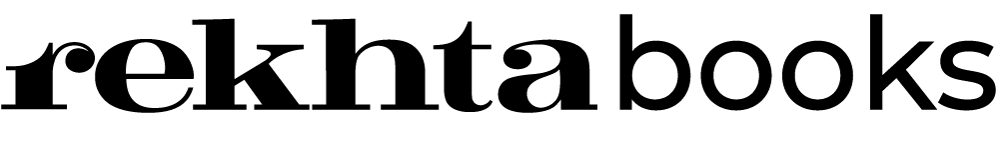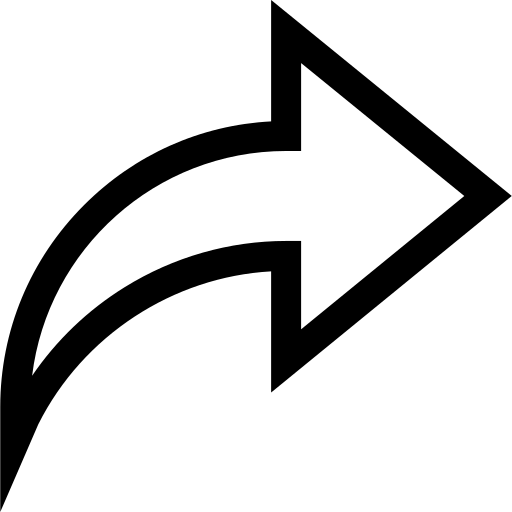भवानीप्रसाद मिश्र की कविता में पेड़-पौधे, नदियाँ आदि के रूप में वनस्पति जगत की बहुतायत है। इस बहुतायत के कारण को खोजा जाये तो ज्ञात होगा कि हमारी सांस्कृतिक अवधारणा में ही वनस्पति जगत की 'भरमार निहित रही है। जिस देश के कवियों ने यह कल्पना ही है कि किसी सुन्दरी के मुँह में मदिरा भरकर कुल्ला करा दिया और मौलिश्री फूल उठीं। उस देश के 'प्रकृति भाव' को समझे बिना, उस देश की कविता को भला कौन समझ सकता है। इन पेड़-पौधों को जड़ से रस मिलता है, किसी अव्यक्त स्रोत से इनका पोषण होता है। सूर्य का प्रकाश प्ररोहित करता है, ताप इन्हें ऊपर खींचता है। जल इन्हें गहराई देता है, वायु ब्रह्माण्ड से जोड़ती है। इस सातत्य की प्रक्रिया के प्रवाह से वृक्ष छायादार-फलदार बनता है। ऐसे ही इस कृषिजीवी देश में नदियाँ जीवन की हरियाली हैं और वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में धरती की रक्त प्रवाहिणी सांस्कृतिक नाड़ियाँ हैं। यह चल रही है तो जीवन जल रहा है- यह अविरुद्ध हो रही हैं तो जीवन-प्रवाह में बाधा पड़ रही हैं। मिश्रजी ने कविता में सतपुड़ा के जंगलों को ही नहीं बुलाया, नर्मदा नदी को भी कई रंगों तरंगों में याद किया है। इस नर्मदा का इतिहास परशुराम, कार्तवीर्य एवं सहस्त्रार्जुन से जुड़ा है। एक प्रकार से नर्मदा टकराव और तप की तेजस्वी धारा है। यह टकराव ओर साधना इतनी बढ़ी है कि इसकी चोट से पत्थर 'भवानीशंकर' हो गया है। इसी के रोड़ों से ओंकारेश्वर अवतीर्ण हो गए। इसी नदी ने विक्रमों का पराक्रम देखा है। मालवों, परमारों, कलचुरियों और राष्ट्रकूटों की जय-यात्रा को समझा है। और इसी नर्मदा के किनारे जन्मे हैं-भवानीप्रसाद मिश्र। अतः उनके सांस्कृतिक-बोध को इस नर्मदा ने नियन्त्रित, अनुशासित एवं परिष्कृत किया है। शब्दों की नर्मदा और 'चालीस बरस से डालकर कुटिया' के तमाम अर्थ-सन्दर्भ, जीवन-प्रसंगों के अर्थ इसी बने हैं, इसी में रचे-पचे हैं। नर्मदा के इस सन्त का साबरमती के सन्त से जो वैचारिक लगाव है- उसे भी एक खास सांस्कृतिक आँख से ही देखना-समझना पड़ेगा।