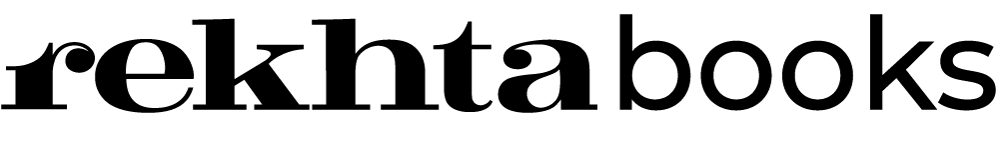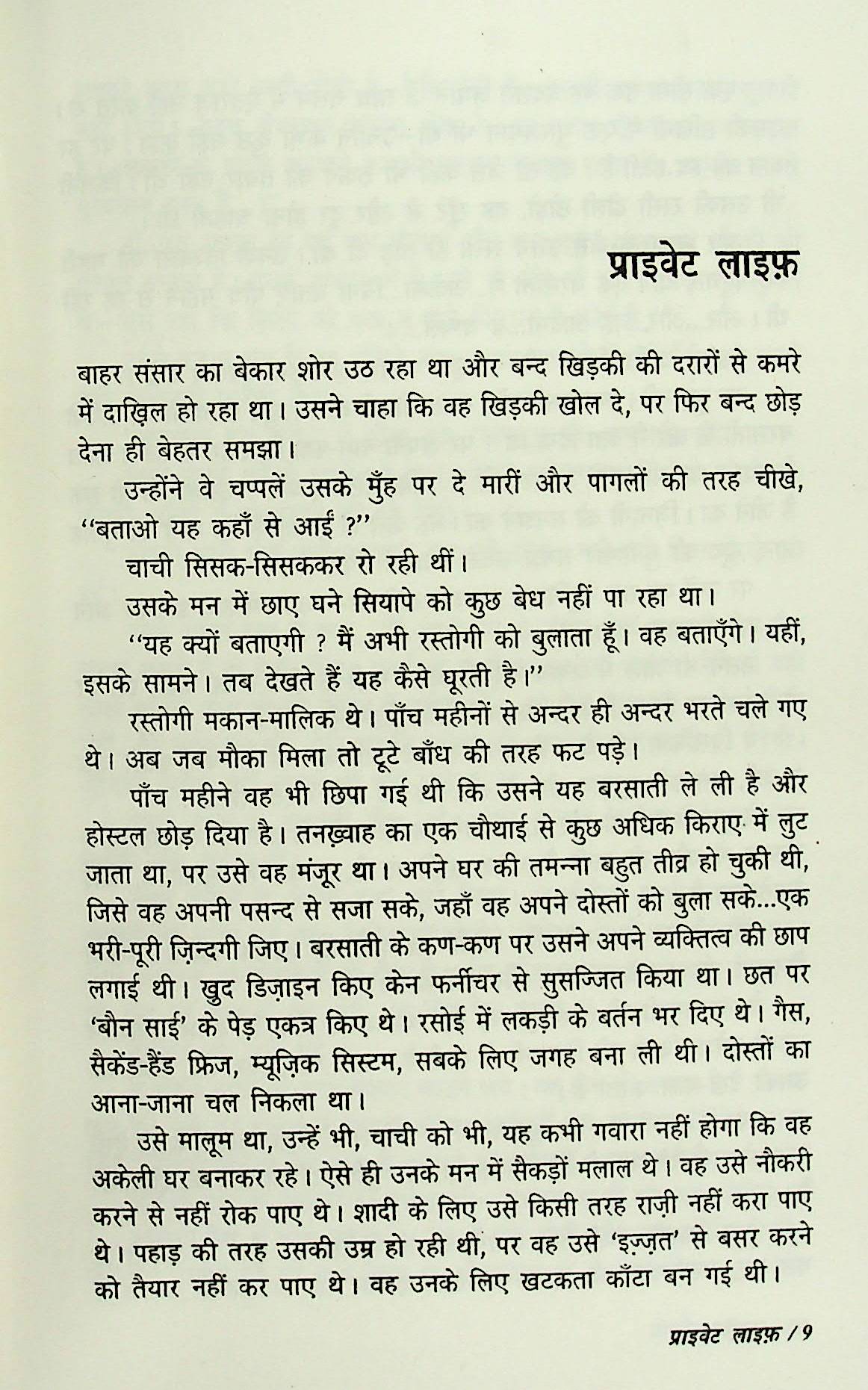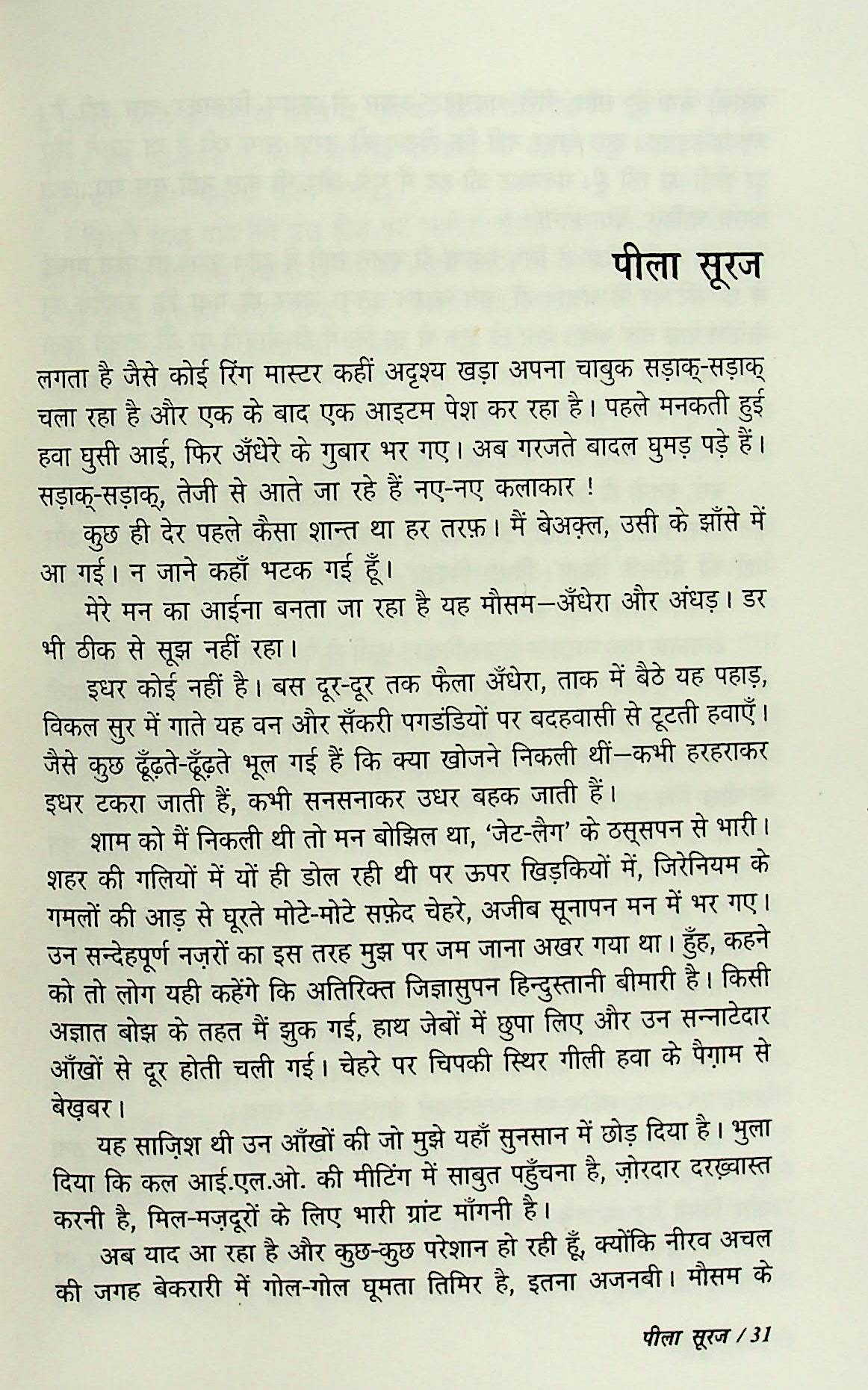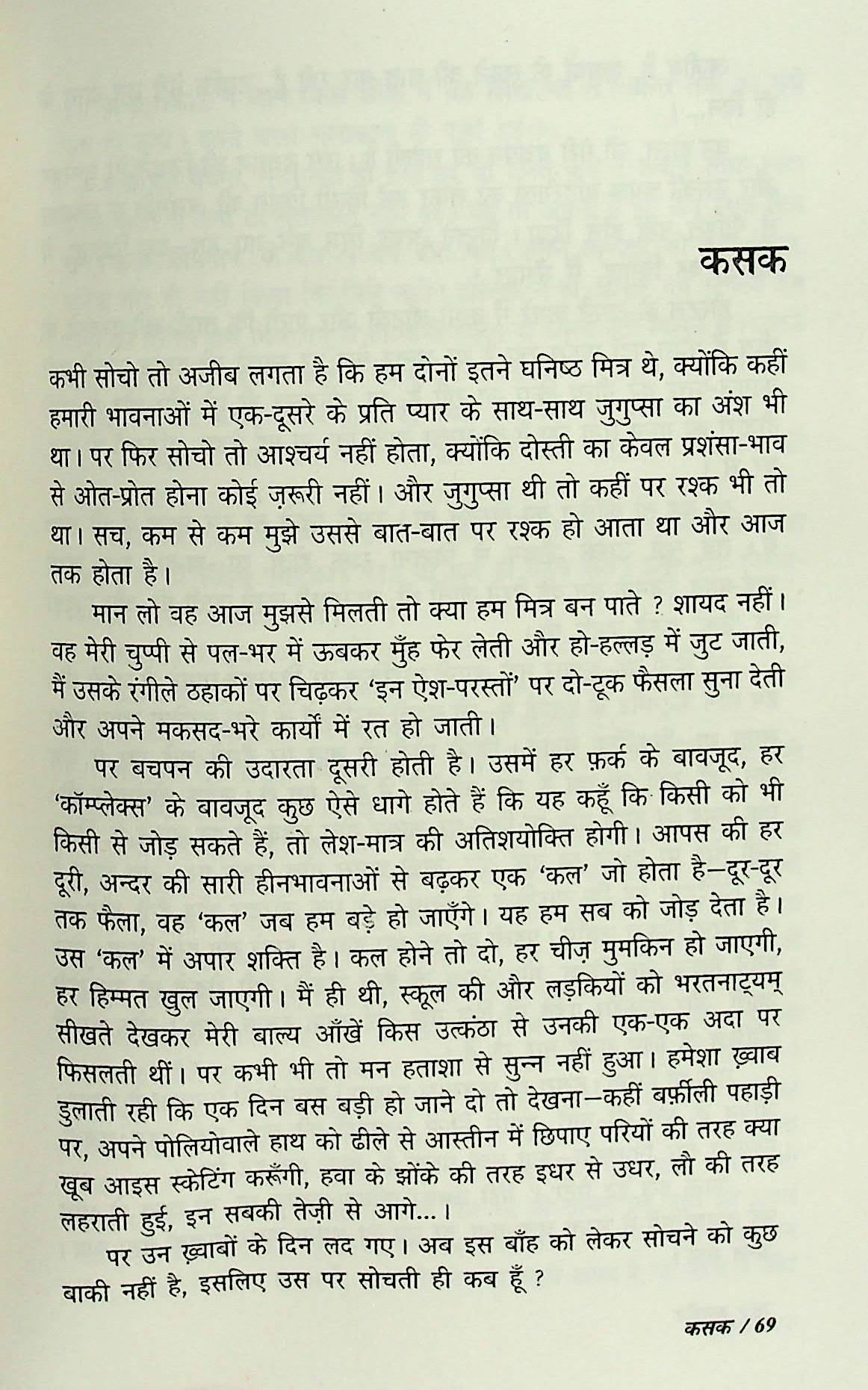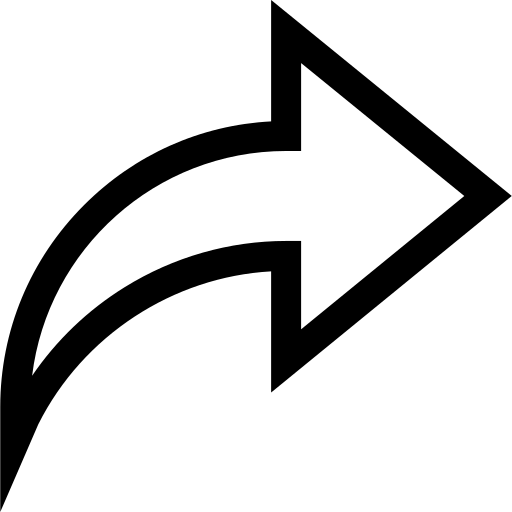क्रम
- प्राइवेट लाइफ़
- बेल-पत्र - 18
- पीला सूरज - 31
- सफ़ेद गुड़हल - 41
- तिनके - 47
- कसक - 69
- दरार - 86
- दूसरा - 96
- हाशिए पर - 108
- अनुगूँज - 129
प्राइवेट लाइफ़
बाहर संसार का बेकार शोर उठ रहा था और बन्द खिड़की की दरारों से कमरे
में दाखिल हो रहा था । उसने चाहा कि वह खिड़की खोल दे, पर फिर बन्द छोड़
देना ही बेहतर समझा।
उन्होंने वे चप्पलें उसके मुँह पर दे मारीं और पागलों की तरह चीखे,
"बताओ यह कहाँ से आईं ?"
चाची सिसक-सिसककर रो रही थीं ।
उसके मन में छाए घने सियापे को कुछ बेध नहीं पा रहा था ।
“यह क्यों बताएगी ? मैं अभी रस्तोगी को बुलाता हूँ। वह बताएँगे। यहीं,
इसके सामने। तब देखते हैं यह कैसे घूरती है ।"
रस्तोगी मकान मालिक थे । पाँच महीनों से अन्दर ही अन्दर भरते चले गए
थे। अब जब मौका मिला तो टूटे बाँध की तरह फट पड़े । बुला
पाँच महीने वह भी छिपा गई थी कि उसने यह बरसाती ले ली है और
होस्टल छोड़ दिया है । तनख़्वाह का एक चौथाई से कुछ अधिक किराए में लुट
जाता था, पर उसे वह मंजूर था । अपने घर की तमन्ना बहुत तीव्र हो चुकी थी,
जिसे वह अपनी पसन्द से सजा सके, जहाँ वह अपने दोस्तों को सके...एक
भरी-पूरी ज़िन्दगी जिए । बरसाती के कण-कण पर उसने अपने व्यक्तित्व की छाप
लगाई थी। खुद डिज़ाइन किए केन फर्नीचर से सुसज्जित किया था। छत पर
'बौन साई' के पेड़ एकत्र किए थे। रसोई में लकड़ी के बर्तन भर दिए थे। गैस,
सैकेंड हैंड फ्रिज, म्यूज़िक सिस्टम, सबके लिए जगह बना ली थी। दोस्तों का
आना-जाना चल निकला था ।
उसे मालूम था, उन्हें भी, चाची को भी, यह कभी गवारा नहीं होगा कि वह
अकेली घर बनाकर रहे । ऐसे ही उनके मन में सैकड़ों मलाल थे। वह उसे नौकरी
करने से नहीं रोक पाए थे। शादी के लिए उसे किसी तरह राज़ी नहीं करा पाए
थे। पहाड़ की तरह उसकी उम्र हो रही थी, पर वह उसे 'इज़्ज़त' से बसर करने
को तैयार नहीं कर पाए थे। वह उनके लिए खटकता काँटा बन गई थी ।
पीला सूरज
लगता है जैसे कोई रिंग मास्टर कहीं अदृश्य खड़ा अपना चाबुक सड़ाक्-सड़ाक्
चला रहा है और एक के बाद एक आइटम पेश कर रहा है। पहले मनकती हुई
हवा घुसी आई, फिर अँधेरे के गुबार भर गए। अब गरजते बादल घुमड़ पड़े हैं।
सड़ाक्-सड़ाक्, तेजी से आते जा रहे हैं नए-नए कलाकार !
कुछ ही देर पहले कैसा शान्त था हर तरफ़ । मैं बेअक्ल, उसी के झाँसे में
आ गई। न जाने कहाँ भटक गई हूँ ।
मेरे मन का आईना बनता जा रहा है यह मौसम - अँधेरा और अंधड़ । डर
भी ठीक से सूझ नहीं रहा ।
इधर कोई नहीं है। बस दूर-दूर तक फैला अँधेरा, ताक में बैठे यह पहाड़,विकल सुर
में गाते यह वन और सँकरी पगडंडियों पर बदहवासी से टूटती हवाएँ।
जैसे कुछ ढूँढ़ते-ढूँढ़ते भूल गई हैं कि क्या खोजने निकली थीं- कभी हरहराकर
इधर टकरा जाती हैं, कभी सनसनाकर उधर बहक जाती हैं ।
शाम को मैं निकली थी तो मन बोझिल था, 'जेट-लैग' के ठस्सपन से भारी ।
शहर की गलियों में यों ही डोल रही थी पर ऊपर खिड़कियों में, जिरेनियम के
गमलों की आड़ से घूरते मोटे-मोटे सफ़ेद चेहरे, अजीब सूनापन मन में भर गए ।
उन सन्देहपूर्ण नज़रों का इस तरह मुझ पर जम जाना अखर गया था । हुँह, कहने
को तो लोग यही कहेंगे कि अतिरिक्त जिज्ञासुपन हिन्दुस्तानी बीमारी है। किसी
अज्ञात बोझ के तहत मैं झुक गई, हाथ जेबों में छुपा लिए और उन सन्नाटेदार
आँखों से दूर होती चली गई । चेहरे पर चिपकी स्थिर गीली हवा के पैग़ाम से बेखबर |
यह साज़िश थी उन आँखों की जो मुझे यहाँ सुनसान में छोड़ दिया है। भुला
दिया कि कल आई.एल.ओ. की मीटिंग में साबुत पहुँचना है, ज़ोरदार दरख्वास्त
करनी है, मिल-मज़दूरों के लिए भारी ग्रांट माँगनी है।
अब याद आ रहा है और कुछ-कुछ परेशान हो रही हूँ, क्योंकि नीरव अचल
की जगह बेकरारी में गोल-गोल घूमता तिमिर है, इतना अजनबी। मौसम के
कसक
कभी सोचो तो अजीब लगता है कि हम दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि कहीं
हमारी भावनाओं में एक-दूसरे के प्रति प्यार के साथ- साथ जुगुप्सा का अंश भी
था। पर फिर सोचो तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि दोस्ती का केवल प्रशंसा-भाव
से ओत-प्रोत होना कोई ज़रूरी नहीं । और जुगुप्सा थी तो कहीं पर रश्क भी तो
था। सच, कम से कम मुझे उससे बात-बात पर रश्क हो आता था और आज
तक होता है।
मान लो वह आज मुझसे मिलती तो क्या हम मित्र बन पाते ? शायद नहीं।
वह मेरी चुप्पी से पल-भर में ऊबकर मुँह फेर लेती और हो हल्लड़ में जुट जाती,
मैं उसके रंगीले ठहाकों पर चिढ़कर 'इन ऐश-परस्तों' पर दो-टूक फैसला सुना देती
और अपने मकसद-भरे कार्यों में रत हो जाती ।
पर बचपन की उदारता दूसरी होती है । उसमें हर फ़र्क के बावजूद, हर
'कॉम्प्लेक्स' के बावजूद कुछ ऐसे धागे होते हैं कि यह कहूँ कि किसी को भी
किसी से जोड़ सकते हैं, तो लेश-मात्र की अतिशयोक्ति होगी । आपस की हर
दूरी, अन्दर की सारी हीनभावनाओं से बढ़कर एक 'कल' जो होता है- दूर-दूर
तक फैला, वह 'कल' जब हम बड़े हो जाएँगे। यह हम सब को जोड़ देता है ।
उस ‘कल’ में अपार शक्ति है । कल होने तो दो, हर चीज़ मुमकिन हो जाएगी,
हर हिम्मत खुल जाएगी। मैं ही थी, स्कूल की और लड़कियों को भरतनाट्यम्
सीखते देखकर मेरी बाल्य आँखें किस उत्कंठा से उनकी एक-एक अदा पर
फिसलती थीं। पर कभी भी तो मन हताशा से सुन्न नहीं हुआ। हमेशा ख़्वाब
डुलाती रही कि एक दिन बस बड़ी हो जाने दो तो देखना- कहीं बर्फीली पहाड़ी
पर, अपने पोलियोवाले हाथ को ढीले से आस्तीन में छिपाए परियों की तरह क्या
खूब आइस स्केटिंग करूँगी, हवा के झोंके की तरह इधर से उधर, लौ की तरह
लहराती हुई, इन सबकी तेज़ी से आगे... ।
पर उन ख़्वाबों के दिन लद गए। अब इस बाँह को लेकर सोचने को कुछ
बाकी नहीं है, इसलिए उस पर सोचती ही कब हूँ ?