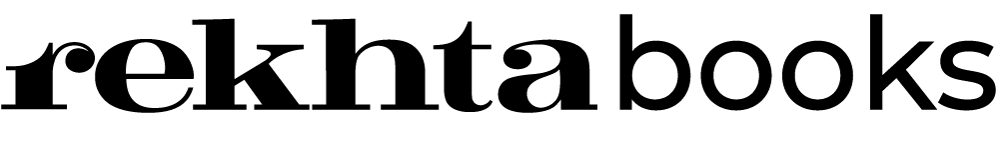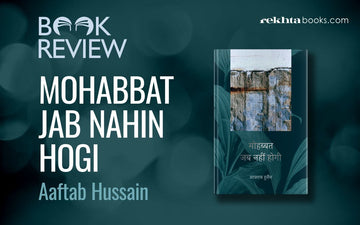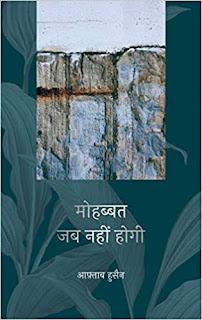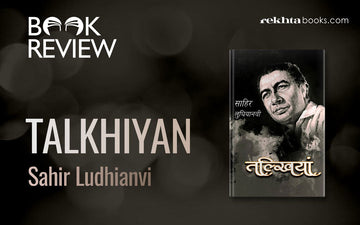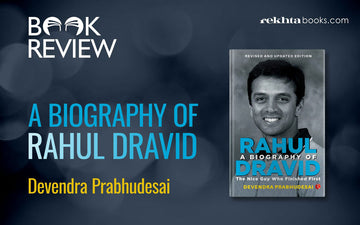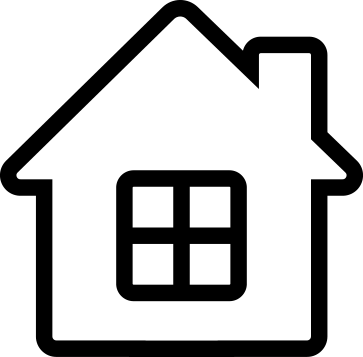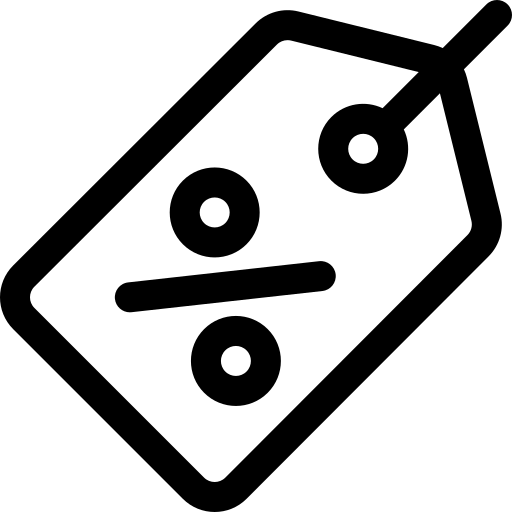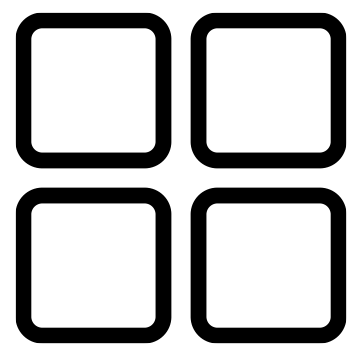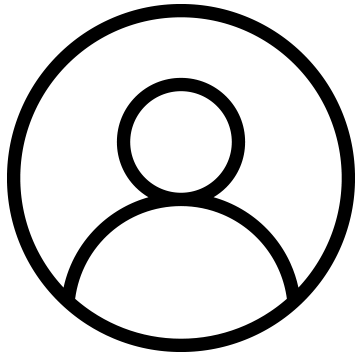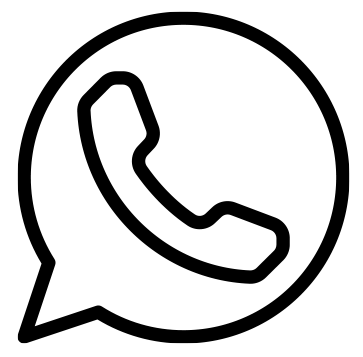पते की बात भी मुँह से निकल ही जाती है
कभी कभी कोई झूठी ख़बर बनाते हुए
*
मिज़ां तक आता जाता है बदन का सब लहू खिंच कर
कभी क्या इस तरह भी याद का काँटा निकलता है
मिज़ां :पलक
*
मैं अपने आप में गुम था मुझे ख़बर न हुई
गुज़र रही थी मुझे रौंदती हुई दुनिया
*
रात बहुत दिन बाद आए हैं दिल के टुकड़े आँखों में
रात बहुत दिन बाद मिले हैं ये अंगारे पानी से
*
रोज़ बुनियाद उठाता हूँ नई
रोज़ सैलाब बहा कर ले जाए
*
कुछ और तर्ह की मुश्किल में डालने के लिए
मैं अपनी ज़िन्दगी आसान करने वाला हूँ
*
न बात कहने की मोहलत है और न सुनने की
चले चलो यूँही एक आध इशारा करते हुए
*
जो भी सच्ची बात कहेगा ज़हर लगेगा दुनिया को
अपने सच में थोड़ा थोड़ा झूठ मिलाते रहा करो
*
कहते हो कि याद उसकी वबाले-ए-दिल-ओ-जाँ है
ऐसा ही अगर है तो भुला कर उसे देखो
वबाले-ए-दिल-ओ-जाँ : दिल और जान की मुश्किल
*
वो यूँ मिला था कि जैसे कभी न बिछड़ेगा
वो यूँ गया कि कभी लौट कर नहीं आया
बात तब की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। आणविक युद्ध की तैयारियों के चलते दोनों देश परीक्षण कर चुके थे। ऐसे में दोनों देशों के तब के प्रधानमंत्रियों ने शांति स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक क़दम उठाया। वो था ,दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू करने का निर्णय। इस बस सेवा को नाम दिया गया 'सदा-ऐ-सरहद' । शुक्रवार 19 फ़रवरी 1999 का दिन भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। इसी दिन दोनों देशों के बीच ये बस यात्रा शुरू की गयी थी जो आज भी दिल्ली और लाहौर के बीच चलती है (बीच में कुछ समय के लिए स्थगित की गयी थी )। भारत की और से इस पहली सद्भावना बस यात्रा में तब के प्रधानमंत्री स्व .श्री अटलबिहारी बाजपेयी जी के साथ भारत के गणमान्य नागरिक भी शामिल थे। वाघा बार्डर पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ़ ने इस बस से पधारे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का भावभीना स्वागत किया था । लाहौर में भारतीयों के सम्मान में हुए एक शाही भोज के कार्यक्रम में श्री नवाज़ शरीफ़ और उनके केबिनेट के सदस्यों और पाकिस्तान के सम्मानित नागरिकों की मौजूदगी में एक युवा शायर ने श्री अटलबिहारी बाजपेयी जी को उन्हीं की कविताओं का उर्दू में छपा संकलन ' हम जंग न होने देंगे' भेंट में दिया। सब ने तालियां बजा कर उस युवा शायर को दोनों देशों की दोस्ती के लिए तैयार किये इस खूबसूरत तोहफ़े के लिए बधाई दी। किसे पता था कि कुछ दिनों बाद ये तोहफ़ा ही इस शायर की जान का दुश्मन बन जायेगा।
हाल हमारा पूछने वाले
क्या बतलाएँ सब अच्छा है
क्या क्या बात न बन सकती थी
लेकिन अब क्या हो सकता है
कब तक साथ निभाता आख़िर
वो भी दुनिया में रहता है
दुनिया पर क्यों दोष धरें हम
अपना दिल भी कब अपना है
दरअसल हुआ यूँ कि इस नौजवान शायर की ये अदा और उसका बाजपेयी जी के साथ मुस्कुराकर फोटो खिंचवाने का मंज़र उस दावत में आये एक फ़ौजी अफ़सर की निग़ाहों में चुभ गया। दूसरे दिन के लगभग सभी पाकिस्तानी अख़बारों में उस शायर, जिसका नाम 'आफ़ताब हुसैन' है, की बाजपेयी जी को क़िताब देते की फोटो प्रमुखता से छपी जो उस फ़ौजी अफ़सर को और भी नाग़वार गुज़री। सीधी सी बात है अगर दुश्मनी ही ख़त्म हो जाय तो फ़ौज का क्या काम ? वैसे भी क़लम से बन्दूक की दुश्मनी बहुत पुरानी है। बन्दूक अवाम की ज़बान बंद करने के काम आती है और क़लम अवाम को ज़बान खोलने को उकसाती है। खैर साहब जैसा कि पड़ौसी मुल्क़ की गौरवशाली परम्परा है, कुछ महीनो के बाद ही फ़ौज ने नवाज़ शरीफ़ की शराफ़त को दरकिनार करते हुए उनकी सत्ता का पासा पलट कर मुल्क़ पर कब्ज़ा कर लिया। आफ़ताब हुसैन की तरफ़ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली इस मासूम सी हरक़त को मुल्क़ के साथ ग़द्दारी समझ कर फ़ौज की तरफ़ से उनपर कड़ी नज़र रखने का फरमान जारी हो गया। जासूस उनकी छोटी बड़ी सभी गतिविधियों को नोट करने लगे। आये दिन उनके उठाये हर क़दम की पूछताछ की जाती जैसे वो फलाँ से क्यों मिले ,क्या बात की फलाँ जगह क्यों गएआदि आदि। एक शरीफ़ बेक़सूर इंसान को परेशान करने के लिए जितने हथकंडे अपनाये जा सकते थे सब अपनाये जाने लगे। उनकी अच्छी खासी सुकून से कट रही ज़िन्दगी दुश्वार की जाने लगी .
समझ में आती नहीं जिसको बात ही मेरी
वो मेरी बात की तफ़्सीर करने के लिए है
तफ़्सीर : व्याख्या
कोई नहीं जो कहे हर्फ़ दो तसल्ली के
जिसे भी देखिये तक़रीर करने के लिए है
*
गुज़र के आया हूँ मैं रौंदता हुआ खुद को
किसी का काम था लेकिन ये काम मुझ से हुआ
*
चलता जाता हूँ मुसलसल किसी वीराने को
और लगता है मुझे जैसे घर आता हुआ हूँ
*
क्या ख़बर मेरे ही सीने में पड़ी सोती हो
भागता फिरता हूँ जिस रोग भरी रात से मैं
*
मोहब्बत है मैं उसको देखता हूँ सोचता हूँ
मोहब्बत जब नहीं होगी तो वो कैसा लगेगा
*
हवस की राह से निकलो अगर नहीं है मोहब्बत
ये रास्ता भी उसी रास्ते से जा मिलेगा
*
रास्ता देखते रहते थे कि आएगा कोई
और जिसे आना था जाने की तरफ़ से आया
*
इस समन्दर में गुज़ारा नहीं होने वाला
किसी खामोश जज़ीरे की तरफ जाता हूँ मैं
*
सर सलामत है तो समझो न सलामत मुझको
अंदर अंदर कोई दीवार दरकती हुई है
पुलिस द्वारा उनसे गाहे बगाहे पूछताछ की जाती, जिरह की जाती, डराया धमकाया जाता और इस मामूली से मसले को फ़ौज के हक़ में ले जाने के लिए उनपर दबाव बनाया जाता कि वो वही कहें जो ख़ुफ़िया एजेंट उनसे कहलवाना चाहते हैं। आफ़ताब हुसैन के जमीर ने पुलिस द्वारा गलत बयानी की पेशकश को मंज़ूर नहीं किया। जमीर पर अपनी किताब 'अघोषित आपातकाल' में कमलेश्वर लिखते हैं कि ' जमीर नाम की कोई चीज फ़ौज के पास नहीं होती जमीर नाम का बीज 'तहजीब-संस्कृति' के खेतों से उगता है। बारूद के गोदामों या बारूदी ज़मीन में नहीं। "
2 मार्च 2002 को कराची में एक मुशायरा आयोजित किया गया था जिसमें शिरकत करने को आफ़ताब लाहौर से कराची गए और मुशायरे के बाद किसी काम की वजह से वहीँ रुक गए। चार मार्च को उनके लाहौर वाले घर पर छापा पड़ा और सारा सामान तहस नहस कर दिया गया। असल में फ़ौजी और आई एस आई के एजेंट आफ़ताब हुसैन को गिरफ़्तार करने को आये थे। ये तो अच्छा हुआ कि वे उस वक्त कराची में थे। कराची में आफ़ताब को उनके छोटे भाई से इस छापे की ख़बर मिली और इससे पहले कि कराची में उनपर आफत टूटती वो अपने गाँव चले गए।
सोचने से ही परेशानी है
मत परेशान रहो, सोचो मत
मन्ज़िल-ए-शौक़ किसे मिलती है
बस यूँही चलते चलो, सोचो मत
इश्क़ का का काम है सुब्हान-अल्लाह
सोचते क्या हो करो, सोचो मत
सोचते रहने से क्या होता है
उठ के कुछ काम करो, सोचो मत
गाँव से इस्लामाबाद जाने और वहां से भारत का वीसा प्राप्त करने की अलग ही कहानी है। वीसा मिलने के बाद अगर आफ़ताब हवाई जहाज़ से भारत आते तो एयरपोर्ट पर ही पकडे जाते लिहाज़ा उन्होंने 'समझौता एक्प्रेस' से जाना ही बेहतर समझा। वाघा बार्डर पर चेकिंग हुई लेकिन वहां की पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं नहीं थी कि उन्हें पकड़ती। पाकिस्तानी ख़ुफ़िया पुलिस को भी उनके भारतीय वीसा की भनक नहीं लगी थी इसलिए वो सकुशल भारत आ गए जहाँ उन्हें राजनीतिक शरण मिल गयी। भारत में उनके बहुत से चाहने वाले और दोस्त थे जिनमें कमलेश्वर प्रमुख थे। कमलेश्वर ने ही उनकी इस दास्तान को अपनी किताब 'अघोषित आपातकाल' में विस्तार से कलम बद्ध किया है। आज हम उनकी ग़ज़लों की किताब 'मोहब्बत जब नहीं होगी' को आपके सामने लाये हैं । इस क़िताब को 'रेख़्ता बुक्स' ने प्रकाशित किया है आप ये किताब उन्होंने 'कमलेश्वर और केदार सिंह' को याद करते हुए समर्पित की है।
चार साँसे थीं मगर सीने को बोझल कर गईं
दो क़दम की ये मसाफ़त किस क़दर भारी हुई
मसाफ़त :दूरी
एक मंज़र है कि आँखों से सरकता ही नहीं
एक साअ'त है कि सारी उम्र पर तारी हुई
साअ'त : पल
किन तिलिस्मी रास्तों में उम्र काटी आफ़ताब
जिस क़दर आसाँ लगा उतनी ही दुश्वारी हुई
आफ़ताब हुसैन का जन्म 6 जून 1962 को तालागंग, पंजाब पाकिस्तान में हुआ। गाँव में शुरूआती तालीम के बाद ये लाहौर पढ़ने चले आये और यूनिवर्सिटी ओरियंटल कॉलेज लाहौर से उर्दू साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसी शहर में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पर काम करते रहे। उनकी क़ाबलियत के चलते उन्हें 'हल्क़ा ए अर्बाबे ज़ौक़' लाहौर का सेकेट्री बनाया गया। यहाँ आपको बतलाता चलूँ कि 'हल्क़ा ए अर्बाबे ज़ौक़' 29 अप्रेल 1939 को पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक मूवमेंट था जिसे 'नून मीम राशिद' और 'मीरजी' ने शुरू किया और बाद में इसमें पाकिस्तान के प्रसिद्ध साहित्यकारों के अलावा भारत के 'कृष्ण चन्दर' और 'राजेंद्र सिंह बेदी' जैसे साहित्यकारों भी जोड़ा। लाहौर से शुरू हुआ ये मूवमेंट अब पाकिस्तान के विभिन्न शहरों के अलावा 'भारत , यूरोप और नार्थ अमेरिका के बहुत से शहरों में भी शुरू हो चुका है। बीस साल की उम्र याने सन 1982 में ही आफ़ताब हुसैन ने अपनी शायरी की बदौलत पाकिस्तान में वो मुक़ाम हासिल कर लिया था जिसे हासिल करने में दूसरे अपनी पूरी उम्र खर्च कर देते हैं।
कोई नहीं जो वरा-ए-नज़र भी देख सके
हर एक ने उसे देखा है देखने के लिए
वरा-ए-नज़र: आँखों की पहुँच से बाहर
बदल रहे हैं ज़माने के रंग क्या क्या देख
नज़र उठा कि ये दुनिया है देखने के लिए
गुज़र रहा है जो चेहरे पे हाथ रक्खे हुए
ये दिल उसी को तरसता है देखने के लिए
पाकिस्तान में आफ़ताब साहब की ज़िन्दगी सुकून से कट रही थी तभी वो हादसा हुआ जिसका ज़िक्र ऊपर किया जा चुका है। भारत में शरण लेने के कुछ अरसे बाद वो अदीबों के आलमी इदारे (P. E. N. ) की दावत पर जर्मनी चले गए और वहाँ से ऑस्ट्रिया की कल्चरल मिनिस्ट्री और विएना शहर के बुलावे पर 'राइटर इन रेसिडेंस ' के तहत वहीँ बस गए। विएना यूनिवर्सिटी से तुलनात्मक साहित्य में पी एच डी की डिग्री लेने के बाद अब उसी यूनिवर्सिटी में दक्षिणी एशिया के साहित्य और संस्कृति का अध्यापन करते हैं और वहां से एक जर्मन-इंग्लिश भाषा की पत्रिका वर्ड एंड वर्ल्ड' भी निकालते हैं. हिंदी के अलावा उनकी रचनाएँ इटेलियन ,इंग्लिश ,पर्शियन, बंगाली और जर्मन आदि कई भाषाओँ में पढ़ी एवं सराही जाती हैं। ग़ज़ल के अलावा वो विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर विचारोत्तेजक लेख भी लिखते हैं। किसी ने सही कहा है कि ज़िन्दगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है अगर वो बाजपेयी जी की कविताओं की उर्दू में किताब न छपवाते और उन्हें स्वयं भेंट न देते तो शायद वो वहाँ नहीं होते जहाँ आज हैं।
कार-ए-दुनिया कहीं निमटा है किसी से भी कहीं
आप बेकार मुसीबत में, पड़े रहते हैं
कार-ए-दुनिया: दुनिया के काम
शेर का नश्शा भी अफ्यून से कुछ कम तो नहीं
कि जो पड़ जाते हैं इस लत में, पड़े रहते हैं
अफ्यून: अफ़ीम
यार लोग आ के सुना जाते हैं बातें क्या क्या
और हम हैं कि मुरव्वत में, पड़े रहते हैं
अब तो पड़ने में कोई लुत्फ़ न रहने में मज़ा
बस पड़े रहने की आदत में, पड़े रहते हैं
यूँ तो आफ़ताब हुसैन साहब की अलग अलग विषयों पर अब तक आधा दर्ज़न से अधिक किताबें उर्दू इंग्लिश में छप कर बाजार में आ चुकी हैं लेकिन उर्दू में छपी उनकी ग़ज़लों की एकमात्र किताब 'मत्ला' 1999 में छपी थी जो भारत और पाकिस्तान में बहुत चर्चित रही. आफ़ताब हुसैन इस क़िताब की भूमिका में लिखते हैं कि " शेर कहना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है कि ये अभिव्यक्ति का वो माध्यम है जो मेरी ऊर्जा को जीनलाइज़ करता है। शेर कहते हुए मेरी नज़रों में कोई विशेष पाठक नहीं होता, मैं खुद भी नहीं होता। बस एक तरंग होती है जो मुझसे लिखवाये चली जाती है। मेरी शाइरी का विषय-वस्तु क्या है ? मैंने इसके बारे में कभी गौर नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ज़िन्दगी ही की तरह शाइरी भी एक फैली हुई क़ायनात है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं अपना सच लिखता हूँ और अपनी पूरी कुव्वत के साथ लिखता हूँ। "
मेरी गुज़ारिश है कि आप आफ़ताब हुसैन साहब को पढ़ें और फिर खुद फैसला करें कि उनकी शाइरी कैसी है। आखिर में उनकी एक ग़ज़ल के चंद शेर आपकी ख़िदमत पेश करते हुए विदा लेता हूँ :
मन्ज़िल हाथ नहीं आ पाती ख़्वाब अधूरा रह जाता है
राह-ए-तलब पर चलते चलते आदमी आधा रह जाता है
राह-ए-तलब: ख्वाहिशों की राह
कभी कभी तो दिल की धड़कन बंद भी हो जाती है साहब
कभी कभी तो सीने में बस दर्द धड़कता रह जाता है
तुझको भूल चुके हैं हम भी लेकिन ऐसी बात नहीं कुछ
सूरज डूब भी जाए अगर तो एक धुँदलका रह जाता है
वक़्त का पहिया चले तो फिर कब चल सकता है ज़ोर किसी का
आदमी अपने आप को क्या क्या चीज़ समझता रह जाता है
- नीरज गोस्वामी