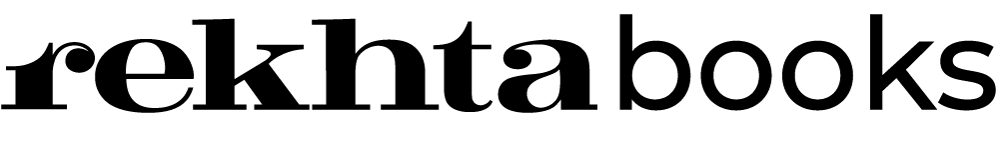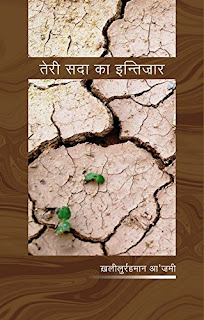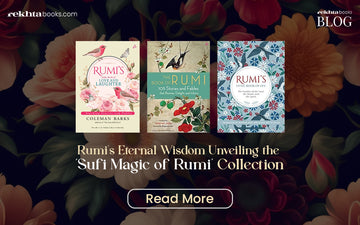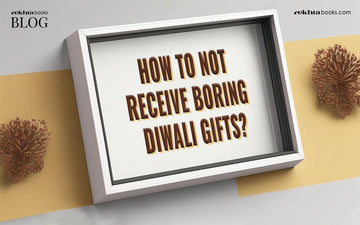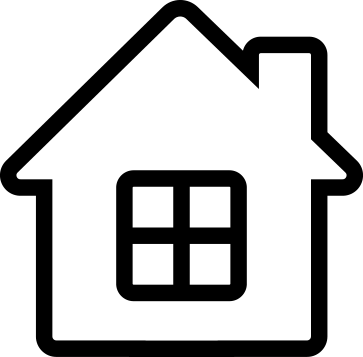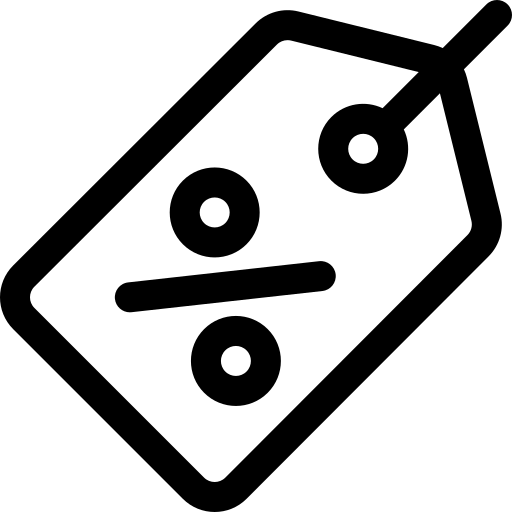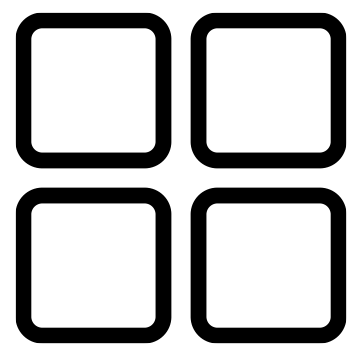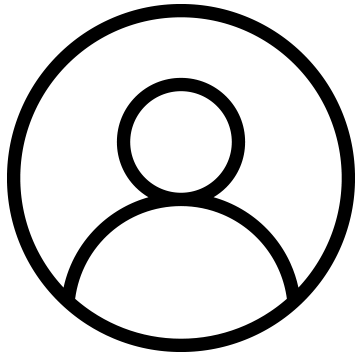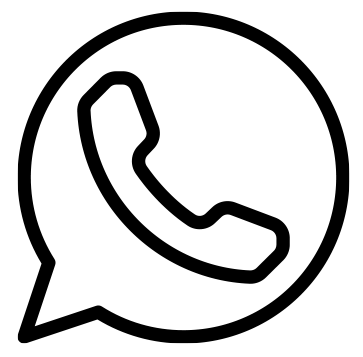सोना लेने जब निकले तो हर हर ढेर में मिट्टी थी
जब मिट्टी की खोज में निकले सोना ही सोना देखा
***
मैं तो घर में अपने आप से बातें करने बैठा था
अन देखा सा इक चेहरा दीवार पे उभरा आता है
***
प्यासी बस्ती प्यासा जंगल प्यासी चिड़िया प्यासा प्यार
मैं भटका आवारा बादल किस की प्यास बुझाऊं
***
अगर घर से निकलें तो फिर तेज धूप
मगर घर में डसती हुई तीरगी
***
हैंं कुछ लोग जिनको कोई ग़म नहीं
अ'जब तुर्फ़ा ने'मत है ये बेहिसी
तुर्फ़ा: अनोखी, बेहिसी:संवेदनहीनता
***
न जाने किस की हमें उम्र भर तलाश रही
जिसे क़रीब से देखा वह दूसरा निकला
***
ये दिल का दर्द तो साथी तमाम उम्र का है
ख़ुशी का एक भी लम्हा मिले तो उससे मिलो
***
घर में बैठे सोचा करते हमसे बढ़कर कौन दुखी है
इक दिन घर की छत पे चढ़े तो देखा घर-घर आग लगी है
***
मुझको नींद नहीं आती है
अपनी चादर मुझे उढ़ा दो
***
बस इतनी बात थी कि अ'यादत को आए लोग
दिल के हर इक जख़्म का टाँका उधड़ गया
अ'यादत:मिज़ाज पुर्सी
***
ऐसी रातें भी हम पे गुज़री हैं
तेरे पहलू में तेरी याद आई
***
इस की तो दाद देगा हमारा कोई रक़ीब
जब संग उठा तो सर भी उठाते रहे हैं हम
1947 की बात है दिल्ली स्टेशन पर गजब की भीड़ थी .दोस्त की सलाह पर वो लड़का दिल्ली से अलीगढ़ वाली ट्रेन में बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया था. उस वक्त देश आजाद होने पर जश्न के रूप में बेगुनाह लोगों का खून सिर्फ़ इसलिए बहाया जा रहा था कि उनके मज़हब अलग थे. बीस साल का ये युवा दुबला पतला सा लड़का सहमा सा एक कोने में बैठा था कि दो-चार स्टेशन के बाद ही कुछ बलवाई ट्रेन में चढ़ गए और एक मज़हब विशेष के लोग ढूंढ कर ट्रेन के बाहर उतारने लगे. लड़के की आंखों में उतरे डर को देखकर एक बलवाई ने उसे गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए नीचे उतार लिया.
अल्लामा इकबाल ने गलत ही कहा था "कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना" जब कि इतिहास गवाह है कि "मज़हब ने ही सिखाया आपस में बैर रखना". हम सिर्फ इस बात पर किसी का खून कर देते हैं कि वो हमारे मज़हब का नहीं है जबकि उसका न तो उस मज़हब में पैदा होने पर कोई इख्तियार होता है न हमारा इस मज़हब में पैदा होने पर. इंसान अकेला इतना हिंसक नहीं होता जितना वो भीड़ में हो जाता है.अकेले में किए गुनाह का बोझ दिल पर अधिक होता है जबकि भीड़ में किए गुनाह का बोझ भीड़ में बंट कर हल्का हो जाता है.
आखरी आवाज़ जो उस लड़के ने सुनी वो थी "मारो" और उसके बाद उसने खंजर अपनी पसलियों में तेजी से घुसता महसूस किया.
मैं ढूंढने चला हूं जो खुद अपने आप को
तोहमत ये मुझ पे है कि बहुत खु़द-नुमा हूं मैं
जब नींद आ गई हो सदा ए जरस को भी
मेरी ख़ता यही है कि क्यों जागता हूं मैं
सदा ए जरस : कारवाँ की घंटियों की आवाज़
लाऊं कहां से ढूंढ कर मैं अपना हम-नवा
खुद अपने हर ख़याल से टकरा चुका हूं मैं
ऐ उम्र ए रफ़्ता मैं तुझे पहचानता नहीं
अब मुझको भूल जा कि बहुत बेवफा़ हूं मैं
ज़ख्म कितना भी गहरा हो भर जाता है ।रह जाता है सिर्फ़ एक निशान जो हमेशा इस बात की याद दिलाता है कि कभी यहां एक ज़ख्म था। हमारे आज के शायर ख़लीलुर्रहमान आ'ज़मी जिनकी किताब "तेरी सदा का इन्तिज़ार" का जि़क्र कर रहे हैं इस निशान को कभी नहीं भूल पाए. ये निशान हमेशा उनकी आँखों के सामने रहा नतीजतन वो हमेशा अकेलेपन के समंदर में डूबे रहे, खलाओं में भटकते रहे और अपने भीतर टहलते रहे. रस्मन तौर पर वह दुनिया से जुड़े दिखाई जरूर देते थे लेकिन हक़ीक़त में शायद उनका खुद से भी राबता कम था.
जिंदगी आज तलक जैसे गुजारी है न पूछ
जिंदगी है तो अभी कितने मजे और भी हैं
***
यूं जी बहल गया है तेरी याद से मगर
तेरा ख्याल तेरे बराबर ना हो सका
***
भला हुआ कि कोई और मिल गया तुमसा
वगरना हम भी किसी दिन तुम्हें भुला देते
***
ये और बात कहानी सी कोई बन जाए
हरीम ए नाज़ के पर्दे हवा से हिलते हैं
हरीम ए नाज़ :माशूका का मकान
***
हमने उतने ही सर ए राह जलाए हैं चराग़
जितनी बर्गश्ता ज़माने की हवा हमसे हुई
बर्गश्ता: बिगड़ी हुई
***
एक दो पल ही रहेगा सब के चेहरों का तिलिस्म
कोई ऐसा हो कि जिसको देर तक देखा करें
***
मेरे दुश्मन न मुझको भूल सके
वरना रखता है कौन किसको याद
***
सुना रहा हूं उन्हें झूठ मूठ इक किस्सा
कि एक शख्स मोहब्बत में कामयाब रहा
***
हाय वो लोग जिनके आने का
हश्र तक इंतजार होता है
***
इतने दिन बीते कि भूले से कभी याद तेरी
आए तो आंख में आंसू भी नहीं आते हैं
***
खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहने दो
दिल में महताब उतरता है इसी जीने से
***
जिंदगी छोड़ने आई मुझे दरवाजे तक
रात के पिछले पहर मैं जो कभी घर आया
***
उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ और उस के आस पास ख़ास तौर पर सुल्तानपुर इलाक़े की मिटटी में पता नहीं क्या तासीर है की वहां एक से बढ़ कर एक बेहतरीन शायर हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। ख़लीलुर्रहमान साहब की पैदाइश भी सुल्तानपुर के गाँव सीधा की है। गाँव के कट्टर मुस्लिम परिवार में मोहम्मद सफी साहब के यहाँ 1927 में आज़मी साहब का जन्म हुआ। आजमगढ़ से मैट्रिक पास करने के बाद अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर 1957 में पी.एच.डी की।
वो दिन कब के बीत गए जब दिल सपनों से बहलता था
घर में कोई आए कि न आए एक दिया सा जलता था
शायद अपना प्यार ही झूठा था वरना दस्तूर ये था
मिट्टी में जो बीज भी बोया जाता था वो फलता था
दुनिया भर की राम कहानी किस किस ढंग से कह डाली
अपनी कहने जब बैठे तो इक इक लफ्ज़ पिघलता था
ख़लील साहब को लिखने का शौक बचपन से ही था बच्चों की पत्रिका "पयामी तालीम" में उनकी रचनाएं नियमित छपती थीं. इस शौक को उन्होंने उर्दू साहित्य को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने में परवान चढ़ाया. गद्य और पद्य दोनों विधाओं में उनकी क़लम चली और खूब चली. पुराने और अपने समकालीन रचनाकारों पर उन्होंने आलोचनात्मक लेख लिखे जो आज भी उर्दू के सर्वश्रेष्ठ आलोचनात्मक लेखों में शामिल होते हैं. उस वक्त जब शायरी महबूब के आरिज़ ओ लब ,बुलबल ओ चमन, हुस्न ओ इश्क की जंजीरों में जकड़ी हुई थी खलिल साहब ने अपने समकालीनों के साथ उसे जदीदियत की ओर मोड़ा. उसे प्रगतिशील बनाया और उसमें वो लफ़्ज इस्तेमाल किए जो अमूमन शायरी की ज़बान से दूर रखे जाते हैं.
और तो कोई बताता नहीं इस शहर का हाल
इश्तिहारात ही दीवार के पढ़ कर देखें
इश्तिहारात: विज्ञापन
जितने साथी थे वो इस भीड़ में सब खोए गए
अब तो सब एक से लगते हैं किसे हम ढूंढें
घर की वीरानी तलब करती है दिन भर का हिसाब
हमको यह फ़िक्र जरा शाम को बाहर निकलें
ब्लड कैंसर एक गंभीर बिमारी है जो ख़लील साहब को उस वक्त लगी जब उनका लेखन उरूज की ओर था. उनके मित्र शमीम हन्फ़ी लिखते हैं कि " देश में चेतना के चराग की लौ रोज़ ब रोज़ तेज होती जा रही थी और इस पूरी जद्द ओ जह्द में ख़लील साहब का हिस्सा सबसे ज्यादा था । वो जदीदियत के क़ाफ़ला-सालारों में शुमार किए जाते थे। अचानक ख़लील साहब की सेहत ज़वाब देने लगी लेकिन बीमारी के दौर में भी वो तख़्लीक़ी ( क्रिएटिव) और फन्नी (आर्टिस्टिक ) सतह पर बहुत ज़रखेज और शादाब दिखाई देते थे। आखरी दौर में लिखी उनकी ग़ज़लों और नज़्मों में आप मौत का रक़्स देख सकते हैं। अपनी और बढ़ती मौत के क़दमों की आहट साफ़ तौर पे रोज़ सुनना मौत से भी बदतर होता है। वो रात में उठकर बैठ जाते और जल्दी जल्दी हमेशा पास ही रखे काग़ज़ पर लिखने लगते। उस दौर में लिखी रचनाओं में अधूरे रह गए ख़्वाबों का दर्द और उदासी का रंग झलकता है "
एक जून 1978 को मात्र 51 वर्ष की उम्र में ख़लील साहब ने दुनिया ऐ फ़ानी को अलविदा कह दिया।
ये अलग बात कि हर सम्त से पत्थर आया
सर-बुलन्दी का भी इलज़ाम मिरे सर आया
बारहा सोचा कि ऐ काश न आँखें होतीं
बारहा सामने आँखों के वो मंज़र आया
मैं नहीं हक़ में ज़माने को बुरा कहने के
अब के मैं खा के ज़माने की जो ठोकर आया
ख़लील साहब के शागिर्दों में अँगरेज़ उर्दू स्कॉलर रॉल्फ रसेल और शायर 'शहरयार' उल्लेखनीय हैं। उनका तअल्लुक़ बशीर बद्र, ज़ाहिदा ज़ैदी ,मुई'न अहसन जज़्बी ,नासिर काज़मी ,इब्न इंशा ,बलराज कोमल, बाक़र मेहदी जैसे अदीबों से रहा। उनकी लिखी किताबों की एक लम्बी फ़ेहरिस्त है। उनकी किताबों का सफर 'कागज़ी पैराहन" से शुरू हुआ जो 1953 में मंज़र ऐ आम पर आयी उसके बाद 'नया अहद नामा' 'फ़िक्र ओ फ़न' 'ज़ाविये निगाह' आदि दस किताबों से होता हुआ 'ज़िन्दगी ऐ ज़िन्दगी' पर ख़तम हुआ. देवनागरी में उनकी एकमात्र किताब "तेरी सदा का इंतज़ार" 'रेख़्ता बुक्स बी 37 ,सेक्टर -1 नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित हुई। ये किताब अब अमेज़न पर ऑन लाइन उपलब्ध है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ जीते जी किसी को सम्मान देने से परहेज़ किया जाता है इसीलिए ख़लील साहब को उनके जाने के बाद न सिर्फ़ उर्दू साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए ' ग़ालिब अवार्ड' दिया गया बल्कि यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें प्रोफ़ेसर की पदवी भी अता की गयी।
चलते चलते उनकी एक ग़ज़ल ये अशआर भी पढ़वा देता हूँ :
दूर रह कर ही जो आँखों को भले लगते हैं
दिल ए दीवाना मगर उनकी ही क़ुर्बत मांगे
पूछते क्या हो इन आँखों की उदासी का सबब
ख्वाब जो देखे वो ख़्वाबों की हक़ीक़त मांगे
अपने दामन में छुपा ले मेरे अश्कों के चराग
और क्या तुझसे कोई ऐ शब-ऐ-फ़ुर्क़त मांगे
वो निगह कहती है बैठे रहो महफ़िल में अभी
दिल की आशुफ़्तगी उठने की इजाज़त मांगे
आशुफ़्तगी: दीवानगी