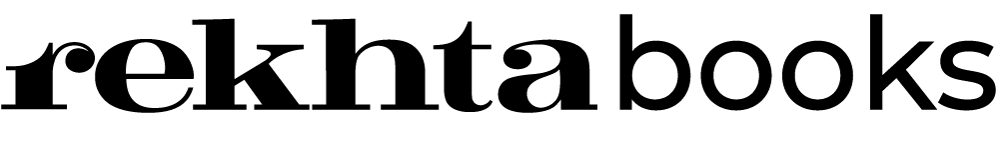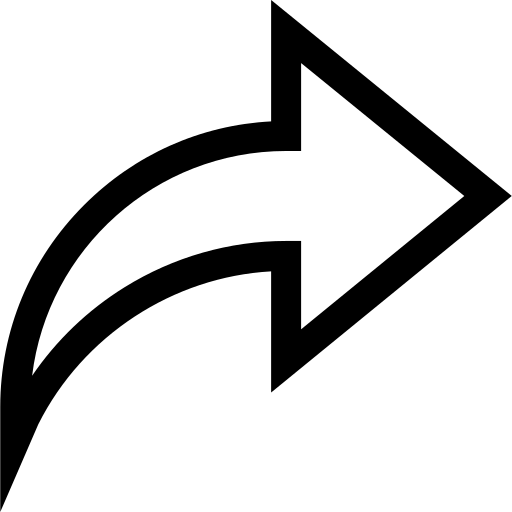लखनऊ
1 अक्तूबर,
1943
अज़ीज़म अख़्तर साहब !
आपको ये अजनबी तहरीर देखकर हैरत होगी और वाक़िफ़यत हासिल
होने पर क्या अहसास पैदा हो इसका अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता।
बहरहाल फे 'ल' अपनी जगह पर जसारतआमेज़' ज़रूर है, इससे मुझे ख़ुद
इनकार नहीं गो कि अमली रौशनी में इसे बड़ी अहमियत हासिल न होनी
चाहिए मगर रिवाज और रिवायात को शायद लरज़ा ही आ जाए मेरा ये
इक़्दाम' देखकर। मगर क्या करूँ कि अक्सर अपने को वहाँ पाती हूँ " जहाँ
पिघली हुई ज़ंजीर आइने - क़दामत की । "
इस मुहमल तम्हीद' के उठाने का मक़सद ये है कि गुज़िश्ता' डेढ़
साल से आपकी जानिब से एक तहरीक' हुई । इस तहरीक पर मुझे तहय्युर
ज़रूर हुआ क्योंकि मुझे एहसास ही नहीं यक़ीन है कि मुझमें कोई ज़ाहिरी
जाज़िबयत' या कशिश ऐसी नहीं जो लोगों को अपनी तरफ़ खींचे। यही
ख़्वाहिशमन्दी" अगर थोड़ी-बहुत वाक़िफ़यत के बाद आपकी तरफ़ से होती तो
मुस्लिम गर्ल्स कालिज
अलीगढ़
28 अप्रैल, 1945
अख़्तर मेरे,
बहुत से प्यार,
तुम्हारा ख़त कल शाम मुझ तक पहुँचा । महमूद साहब के मकान से
इस घर का फ़ासला काफ़ी है, जब कोई आ निकलता है तो ख़त साथ लेता
आता है। बहरहाल ख़ैरियत मालूम करके इत्मीनान हुआ ।
यहाँ के हालात : फ़य्याजी दगा दे गई। सूरत ये है कि चौबीस घंटे
की ग़ुलामी है और मैं। लखनऊ तुम गए थे तो तुमने देखा था कि इस बच्चे
की मसरूफ़ियत' ने किस तरह तौबा भुला रखी थी, गो कि मेरे बराबर की
मददगार अम्माँ थीं। फिर मकान के तमाम नौकर मौजूद थे- यहाँ आपा
बीमार और नफ़ीस इम्तेहान में मुब्तला' । मैं हूँ और जादू की मुसीबत। अब
जिस तरह हो सके तुम कहीं से नौकर तलाश करके लाओ, वरना मैं तो
मर जाऊँगी अख़्तर। आगरा की मुलज़िमा ही खिलाने के लिए मिल जाए
तो ग़नीमत है।
भोपाल
24 जनवरी, 1950
अज़ीज़ अख़्तर !
आज कई दिन हो गए, न मैंने ही तुम्हें ख़त लिखा और न तुम्हारी
कोई तहरीर आई ।आजकल एहसासात इस तरह कुचले हुए महसूस होते हैं कि क़लम
उठाने की सकत' भी पैदा नहीं होती, बस वक़्त के धारे पर बेइख़्तियार' बहे
जा रही हूँ, कोशिश और इरादे के बग़ैर । बा'ज़ वक़्त तो जुनून पैदा होने
लगता है । फिर सोचती हूँ कि मैं माँ हँ दो बच्चों की । और मुझे जामे नाक़िस
है तुम्हारी ज़िन्दगी में बेहतरी के इज़ाफ़े का, फिर क्या ये तसल्लियाँ काफी
नहीं, लेकिन सच जानो, 'उनसे मिलकर बढ़ गई कुछ और भी बेताबियाँ'
वाला मज़्मून मेरे हक़ में है। तुम्हारे जाने के बाद से साबित हुआ दुरुस्त
भोपाल काटने को दौड़ता है। कब ये तन्हाई का दौर ख़त्म होगा मेरे अल्लाह !
तुम ख़त नहीं लिखते। मेरी ढारस नहीं बँधाते। इस तन्हाई में तुम्हारा
ख़त मेरे ज़िन्दा रहने के लिए हद्दे दर्जा' ज़रूरी है। इस तरह चुप-चुप न
हो जाया करो।
महबूब मंज़िल, भोपाल
17 जुलाई, 1950
10 बजे शब
अख़्तर अज़ीज़!
आज सेहपेहर' तुम्हारी पन्द्रह की लिखी हुई तहरीर मिली। तुम्हारे पिछले
ख़तूत भी मुझे मिल गए थे। गो कि एक ख़त ठेकेदार साहब की बेगम
साहिबा के मुतालेअ' के बाद मुझ तक पहुँच सका, उस पर भी रश्क पैदा है!
के साथ तुमने मुझे ये किताबें भेजी हैं दोस्त! तुम्हारी फ़िज़िकल एट्रेक्शन से
भी हमेशा ख़ुद को कम ही पाया और आज तुम्हारे इस ज़ेहनी लगाव के
बराबर भी खुद को नहीं पाती। तुम्हारी बुलन्दियाँ मैं न छू सकूँगी दोस्त! मैं
वो रिफ़अतें कहाँ से लाऊँ कि तुम्हारे बराबर ख़ुद को कर सकूँ। मैं उन
अछूती बुलन्दियों की पूजा ही कर सकती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे सामने सर
झुकाया है और हमेशा सर ही झुकाऊँगी। तुम बहुत ऊँचे और
हो। और अपनी इस बुलन्दी ही के बाइस हमेशा-हमेशा अनअटैनेबल । तुम्हें
हद से ज़्यादा पा लेने पर भी ये एहसास ग़ालिबन मुझे बाक़ी रहता है कि
बहरहाल, किताबों का पार्सल भी पहुँचा। कैसे प्यार और अनोखी मुहब्बत