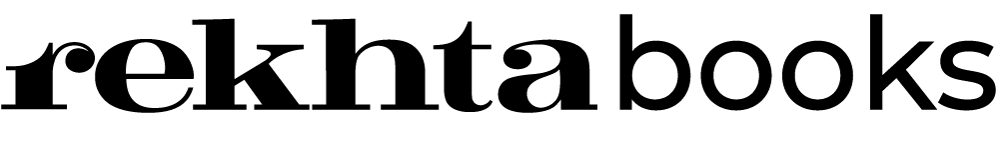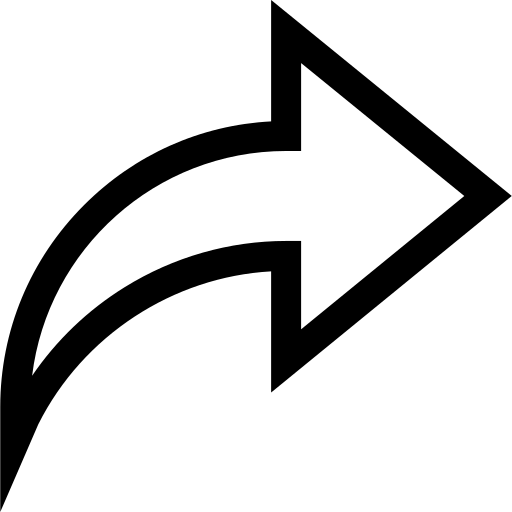क्रम
1. स्याही में सुर्खाब के पंख - 9
2. कत्थई नीली धारियों वाली कमीज - 47
3. चीन्हा - अनचीन्हा - 61
4. सुनयना! तेरे नैन बड़े बेचैन! - 77
5. राग-विराग - 85
6. इन दिनों - 106
7. नीड़ - 115
स्याही में सुर्खाब के पंख
सोनपती बहन जी माचिस लिये रहती हैं
सोनपती बहनजी को भूला नहीं जा सकता था।
वे शिक्षा के सबसे जरूरी पाठ की तरह याद रखने के लिए थीं ।
वे बहुत पहले निकली थीं नौकरी करने, जब औरतें किन्हीं मजबूरियों में
निकलती थीं। वे भी मजबूरी में निकली थीं, ऐसी जनश्रुति थी । जनश्रुति यह
भी थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद चार लड़कियों की जिम्मेदारी और
रिश्तेदारों की हृदयहीनता ने उन्हें नौकरी करने के लिए प्रेरित किया था ।
यह आम भारतीय जीवन का सच जैसा था और इसी रूप में स्वीकृत सच
की तरह भी था।
जोर-शोर से चलाए जा रहे स्त्री-शिक्षा के अभियान के चक्कर में उन्हें घर
से पकड़कर एक रोज स्कूल में बैठा दिया गया था। स्कूल एक सेठ और उनकी
पत्नी ने शुरू किया था । इस कन्या पाठशाला के लिए हर हाल में लड़कियाँ
चाहिए थीं। वे लोग यानी कि सेठ और सेठानी खुद चलकर उन घरों में गए थे,
जहाँ लड़कियाँ शिक्षा के उजाले से दूर अँधेरे कोने में खड़ी अपने से छोटे बच्चों
की नाक पोंछ रही थीं, टट्टी धो रही थीं, बरतन माँज रही थीं, रोटी थाप रही
थीं। कहीं-कहीं घास काटने गई थीं, कहीं गोबर पाथ रही थीं। ऐसे में उन्होंने
समझाया कि शिक्षा के उजाले से कैसे घास और गोबर की गन्हाती दुनिया से
निकलकर बल्ब की धवल रोशनी में आया जा सकता है- ? सोनपती, जो
आगे चलकर बहनजी बनीं, स्कूल नहीं जाना चाहती थीं। वहाँ की हर क्षण
रखी जानेवाली नजर से बड़ी कोफ्त होती थी, लेकिन उन्हें पकड़कर ले जाया
कत्थई नीली धारियों वाली कमीज
एक ही मन के भीतर कई-कई मन छिपे होते हैं, दिखते नहीं। हम जानते
तक नहीं उनका होना ! कितने कुछ का होना हम नहीं जानते ! जो जान
जाते हैं, उसे भी कहाँ जानते हैं! कह लें कि कितना जानते हैं? यह तो मन की
बात थी। वह सौ पर्दों में छिपा लगता था, तो एकदम साफ सामने भी लगता
था। उसे जान - जानकर भी नहीं जानते थे ! जब पकड़ते भी तो एक को पकड़
पाते, उसे ही पूरा मान लेते ! लेकिन न जाने कहाँ से उस वक्त एक दूसरा ही रूप
नमूदार होकर चौंका देता, जबकि लग रहा होता कि मन टूट-फूटकर ध्वस्त,
धूमिल हो चुका है और अब कभी भी, कत्तई कोई फुनगी यहाँ नहीं फूटनेवाली ।
तभी, बिल्कुल तभी वह एक दूसरा किसी ओझल दरवाजे की फाँक से
झाँक-झाँककर मुस्करा उठता है। उसी फाँक से एक हल्की-सी रोशनी चली
आती है। सहसा झपटकर एक मन उसे उठा लेता है।
एक मन समझाता है, एक मन रोकता है, तो दूसरा तोड़-फोड़ देना चाहता
है, फ्रेम में अनफिट, निकल भागना चाहता है उन्मुक्त आकाश में!
एक मनमयूर नाचता है तो दूसरा इसे निहारता किसी ऐसे वक्त की ताक
में बैठा होता है जब एक करारी चोट मार सके - नृत्यभंग, लास खंडित, राग
तोड़... एक तटबन्ध टूटता है... एक जलस्रोत सूखता है...
तभी बादल गरजते हैं तो मैं चौंककर खिड़की तरफ भागती हूँ । परदा
हटाकर एक और मन से बादलों के बीच कुछ ढूँढ़ने लगती हूँ..." बरसो न
जमकर, बरसो बरखा रानी...
काले-काले बादल ऐसे उमड़कर चले आ रहे हैं... काश ! मैं मोर होती,.
पंख फैलाकर नाचती... अपना दुपट्टा लहरा - लहराकर मैं कुछ हल्का-सा